प्रेमचंद पर लिखित बहुत सारी पुस्तकों-निबंधों को पढ़ते हुए पिछले कुछ वर्षों में निर्मल वर्मा द्वारा प्रेमचंद पर लिखे गए इस निबंध के शीर्षक ने मुझे जितना आकर्षित किया शायद उतना किसी भी शीर्षक ने नहीं। निर्मल वर्मा ने अपने लेख का शीर्षक रखा है ‘प्रेमचंद की उपस्थिति’। एक साहित्यिक अध्येता के रूप में हर लेखक को यह सोचना पड़ता ही है और सोचना भी चाहिए कि प्रेमचंद की उपस्थिति उसकी जिन्दगी में कितनी और कहां-कहां है? निर्मल वर्मा ने भी अपने इस निबंध में यही समझने की कोशिश की है कि प्रेमचंद सिर्फ उनके यहां ही नहीं साहित्य में भी कहां-कहां और कैसे उपस्थित हैं। वैसे इस निबन्ध को गहराई से पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि निर्मल वर्मा साहित्य की परम्परा में प्रेमचंद की उपस्थिति नहीं बल्कि शायद अनुपस्थिति ढूंढ़ने का उपक्रम कर रहे थे। एक साहित्यिक अध्येता के रूप में यदि निर्मल वर्मा भी इस सवाल पर विचार कर रहे होते कि प्रेमचंद उनके जीवन में या साहित्यिक परम्परा में कहां-कहां उपस्थित हैं तो यह एक अच्छी स्थिति होती, परन्तु ऐसा है नहीं। इस आलेख को पढ़ते हुए कई सवाल मन में उठते हैं कि हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द कितने उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित? साहित्य में प्रेमचंद की कौन सी परम्परा है और क्या किसी परम्परा में प्रेमचंद विश्वास रखते हैं? निर्मल ने इस निबंध में माना है कि प्रेमचंद की जिस परम्परा की आज बात हो रही है अगर आज प्रेमचंद जिन्दा होते तो परम्परा की इस सोच से वे नाराज होते।
‘प्रेमचंद की उपस्थिति’ शीर्षक को अगर एक अच्छी सोच के साथ लिखा जाता तो निस्संदेह यह एक बहुत ही सार्थक शीर्षक होता। क्योंकि हिन्दी साहित्य के पुरोधा लेखक के बारे में यह लिखा जाना, सोचा जाना कि वे कहां-कहां और किस तरह उपस्थित हैं बहुत ही मानीखेज होता। परन्तु इस आलेख को पढ़ते हुए साफ पता चलता है कि निर्मल वर्मा ने इस आलेख को एक खास मकसद के लिए लिखा है। आलेख के एकदम शुरुआत में ही लिखा जाता है कि ‘ऐसे समकालीन लेखक भी हैं, जिन्हें शायद प्रेमचन्द का नाम ही निरर्थक जान पड़े- क्योंकि उनकी सृजन-यात्रा में वह उन्हें किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं जान पड़ते, किन्तु ऐसे कथाकारों की रचनाओं में भी हमें प्रेमचन्द की अदृश्य छाया मिल जाती है।’
यह सुनने में हमें बहुत अच्छा लग सकता है कि निर्मल वर्मा प्रेमचन्द की अदृश्य छाया ऐसे लेखकों में भी ढूंढ़ रहे हैं जहां कि प्रेमचंद निरर्थक जान पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लेखक हैं कौन जिनके यहां प्रेमचंद निरर्थक जान पड़ते हैं। प्रशंसक अगर ऐसे हों तो फिर तो निंदकों की जरूरत ही नहीं है। साहित्य में प्रेमचंद की आभा इतनी बड़ी है उसे कम करना आसान नहीं है। इसलिए निर्मल वर्मा धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे अपने मकसद को खोलते भी हैं। निर्मल वर्मा अपनी बात में यहां थोड़ा बचना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने जब यह निरर्थक वाली बात कह दी तो उसकी भरपाई के लिए उन लेखकों में इस अदृश्य छाया वाली बात भी लिख दी। जबकि आगे चलकर वे उस अदृश्य छाया से भी लेखकांे के एक वर्ग को बाहर करते हुए दिखते हैं।
जब यह साबित हो गया कि कुछ साहित्यकार ऐसे भी हैं जिनके यहां प्रेमचंद ‘निरर्थक’ जान पड़ते हैं तब यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिनके यहां प्रेमचंद ‘सार्थक’ जान पड़ते हैं। निर्मल वर्मा ऐसे लेखकों के यहां भी प्रेमचंद की इस ‘सार्थकता’ को ढ़ूंढ़ने की कोशिश करते हैं। निर्मल कहते हैं कि आलोचकों ने एक गजब का भ्रम फैलाया है कि किसी भी लेखक का प्रभाव या उनकी उपस्थिति को ढ़ूंढ़ने के लिए वे उस लेखक के विचार की तरफ चले जाते हैं। जबकि यह सरासर गलत है।
वे लिखते हैं- ‘किसी लेखक की उपस्थिति या प्रभाव को उसके विचारों या विश्वासों में खोजना, जबकि सत्य यह है कि साहित्य में किसी लेखक के विश्वास उनकी रचनाओं में अलग कोई हैसियत नहीं रखते।’ किसी लेखक को उनके विचार से हटाना जब थोड़ा अजीब लग रहा था तब निर्मल वर्मा ने इसे थोड़ा और अधिक स्पष्ट करके बतलाना चाहा। वे आगे लिखते हैं -‘शायद मैं अपनी बात को उलझाकर कह रहा हूं, वास्तव में बात बहुत सरल है-यदि आज हम अपने बीच प्रेमचंद की उपस्थिति महसूस करते हैं- तो उनके प्रगतिशील विचारों या यथार्थवादी आदर्शों (या आदर्शवादी यथार्थ- आप जो भी कहना चाहें) के कारण नहीं-बल्कि उनकी रचनाओं में निहित मनुष्य, एक भारतीय मनुष्य की मानसिक बनावट के कारण, जिसे पगने, फूलने में सैकड़ों वर्ष लगे थे-एक स्थिर व्यक्तित्व का चेहरा जिसका दर्शन हमें पहली बार उनकी कहानियों-उपन्यासों में हुआ था।’ स्पष्ट है जब यहां यह समझाने की कोशिश हो रही है कि प्रेमचंद की उपस्थिति हमारे यहां उनके प्रगतिशील विचारों या यथार्थवादी आदर्शों के कारण नहीं है। तब साफ समझ में आ जाता है कि यह आलेख साहित्य की परम्परा में प्रेमचंद की उपस्थिति नहीं बल्कि अनुपस्थिति ढूंढ़ने की कोशिश है। निर्मल वर्मा जब यह कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वे उलझा कर कह रहे हैं वास्तव में तब तक वे अपनी धारणा बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रेषित कर चुके होते हैं।
यह आलेख वास्तव में प्रेमचंद के यथार्थवादी-प्रगतिशील विचार को फ्यूज करने के लिए लिखा गया है। जब ऊपर वे कह चुके थे कि किसी भी लेखक के यहां विचार की कोई अहमियत नहीं है तब वे अपनी बात को स्पष्ट कर चुके थे। परन्तु प्रेमचंद के कद को छोटा करने के लिए हिम्मत जुटाते-जुटाते निर्मल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे वे प्रेमचंद के पास सीधे आते हैं और कहते हैं कि प्रेमचंद महान तो हैं परन्तु अपनी रचनाओं के कारण, अपने विचार के कारण नहीं। गोया विचार और रचना दोनों दो अलग-अलग चीजें हैं। निर्मल वर्मा के लिए ये तीन शब्द ‘विचार’, ‘प्रगतिशीलता’ और ‘यथार्थ’ एक फांस की तरह हैं। यही वे शब्द हैं जिनसे प्रेमचंद की गरिमा है। इसलिए प्रेमचंद ने इन तीन शब्दों के खिलाफ एक जाल बुना है। पहले उन्होंने एक लेखक की महानता को टैक्स्चुअल साबित किया और टैक्स्ट को विचार से बहुत दूर हटा दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें विचार से कोई दिक्कत नहीं है बस वह साहित्य में ना हो। उन्होंने स्पष्ट कहा ‘मैंने जानबूझकर ‘साहित्य’ में कहा है, क्योंकि उसके बाहर उसके विश्वासों का अवश्य महत्व होता होगा।’ विचार जब तक बाहर है निर्मल वर्मा को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब विचार साहित्य में होगा तब प्रेमचंद की आभा को कम करना संभव नहीं है। इन तीन शब्दों से छुटकारा पाते-पाते निर्मल अपने पसंद के शब्द तक पहुंचते हैं और वह है -‘भारतीयता’। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रेमचंद महान इसलिए नहीं थे कि उनके यहां यथार्थवादी विचार था बल्कि वे महान इसलिए थे कि उन्होंने अपने यहां भारतीय मनुष्य की मानसिक बनावट को सामने लाकर प्रस्तुत किया। सिर्फ मनुष्यता भी कहते तो काम चल सकता था परन्तु निर्मल वर्मा ने इसे भारतीयता से जोड़कर अपनी मंशा स्पष्ट की है। सोचने वाली बात है कि भारत का लेखक है तो भारतीय मनुष्य की ही तो मानसिक बनावट को ग्राफ करेगा ना। उस पर तुर्रा यह कि अगर भारतीय मनुष्य की मानसिक बनावट को रच रहे थे तो क्या यह बगैर विचार के संभव है? मनुष्य की जब मानसिक बनावट को प्रस्तुत किया जाएगा तो यथार्थ उससे इतर और क्या होता है? बस यथार्थवाद को स्वीकृति नहीं देनी है तो नहीं देनी है।
निर्मल वर्मा द्वारा लिखित निबंध ‘प्रेमचंद की उपस्थिति’ को अगर बहुत गम्भीरता से नहीं पढ़ा जाए तो प्रथम दृष्ट्या ऐसा महसूस होगा जैसे यह निबंध प्रेमचंदोत्तर काल के एक बड़े रचनाकार ने अपने से वरिष्ठ रचनाकार की प्रशंसा में लिखा है। परन्तु सच में ऐसा है नहीं। निर्मल वर्मा इस आलेख के सहारे न सिर्फ प्रेमचंद को कम करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि समानान्तर रूप से अपने लिए एक पंक्ति भी तैयार कर रहे थे। इस आलेख में निर्मल का संकोच देखने लायक है। वे लिखते हैं ‘कहते हैं उन्नीसवीं शताब्दी का रूसी साहित्य गोगोल के ‘ओवरकोट’ से बाहर आया था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, किन्तु हिन्दी के आधुनिक कथा साहित्य का बड़ा अंश प्रेमचंद के ‘कफन’ से बाहर आया है, यह मुझे जरूर सत्य जान पड़ता है।’ इस पंक्ति को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे निर्मल वर्मा प्रेमचंद के कद को हिन्दी साहित्य के लिए बहुत ऊंचा करके देख रहे हैं। परन्तु अगली ही पंक्ति में जब वे यह लिखते हैं तब उनका संकोच और उनकी मंशा साफ दिख जाती है। वे लिखते हैं ‘पूरा साहित्य नहीं- ऐसे लेखक हैं, जैनेन्द्र, अज्ञेय और अनेक नए लेखक-जो शायद बिना प्रेमचंद के भी अपनी लीक बना सकते- मैं स्वयं शायद ऐसी श्रेणी में आता हूं जिस पर प्रेमचंद का कोई सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई देता।’ अब यहां पर ठहर कर एक बार अगर फिर से इस आलेख की उस पंक्ति को पढ़ लिया जाए जहां उन्होंने यह लिखा कि ‘‘ऐसे समकालीन लेखक भी हैं, जिन्हें शायद प्रेमचन्द का नाम ही निरर्थक जान पड़े- क्योंकि उनकी सृजन-यात्रा में वह उन्हें किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं जान पड़ते।’ तो निर्मल वर्मा द्वारा आलेख की शुरुआत और आखिर तक में एक तारतम्यता बनती हुई सी दिखती है। यहां एक अंदाजा लगाने की कोशिश भी हो सकती है कि जिन लेखकों के यहां प्रेमचंद प्रासंगिक नहीं जान पड़ते हैं, कहीं ये वही तो नहीं हैं। परन्तु सवाल यह है कि निर्मल वर्मा ने जिन लेखकों के नाम यहां प्रेमचंद की परम्परा में नहीं होने में लिए हैं, क्या उन्होंने उन लेखकों से सहमति ली थी। या फिर वे किस आधार पर ऐसा दावा कर रहे हैं? सिर्फ प्रेमचंद की तरह का ही नहीं लिखने से कोई लेखक ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सृजन-यात्रा में प्रेमचंद उनके यहां प्रासंगिक नहीं रह जाएं। सवाल यह है कि इस दावे को स्थापित करने के लिए क्या निर्मल वर्मा के पास कोई ठोस आधार है?
प्रेमचंद, प्रेमचंद का यथार्थ और जैनेन्द्र कुमार
निर्मल वर्मा जिस ‘कफन’ से हिन्दी के बड़े अंश के बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उस ‘कफन’ की सबसे बड़ी विशेषता वास्तव में प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि थी। और निर्मल वर्मा यहां उसी यथार्थवादी दृष्टि की ही बात भी कर रहे हैं। यह इसी निबंध में आगे और भी स्पष्ट होता है। आगे जब निर्मल यह लिखते हैं कि अगर प्रेमचंद आज जीवित होते और जब इस परम्परा की लड़ाई को देखते तब वे खुद कहते ‘भई आप तो मेरी परम्परा में आते हैं लेकिन मैं। मैं कौन सी परम्परा में आता हूं-सेवासदन की परंपरा में या कफन की परम्परा में।’ तब स्पष्ट हो जाता है कि निर्मल सेवासदन से अलग कफन को यथार्थवादी परम्परा में देख रहे हैं। और निर्मल के अनुसार प्रेमचंद की यह यथार्थवादी परम्परा ही है जिससे हिन्दी का बहुत बड़ा अंश निकला है। और यहां तक ही अगर हम निर्मल को पढें तो लगता है कि निर्मल प्रेमचंद की तारीफ करते हुए एक ऐसी परम्परा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हिन्दी साहित्य समृद्ध हुआ है। लेकिन आगे वे अपने असली मुद्दे पर आते हैं।
यहां पहले एक बार फिर पहली बात पर आते हैं कि हिन्दी साहित्य का बड़ा भाग प्रेमचंद के ‘कफन’ से निकला है। निर्मल ने प्रेमचंद के ‘कफन’ से पूरा हिन्दी साहित्य नहीं बल्कि एक बड़े अंश को बाहर आते हुए देखा। बाहर आने को यहां हमें उस परम्परा का अनुसरण करने से लेना चाहिए। निर्मल ने पूरा हिन्दी साहित्य नहीं लिखकर साहित्य के ‘बड़े अंश को’ लिखकर एक भाग को उससे मुक्त भी रखा है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा उन्होंने इसमें जैनेन्द्र, अज्ञेय और खुद अपने आप को रखा है, जिनके यहां प्रेमचंद का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। यानि जो बिना प्रेमचंद के भी अपनी लीक बनाने की क्षमता रखते हैं। यहां तक आते-आते निर्मल का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यानि निर्मल वर्मा प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा से अलग एक ऐसी पंक्ति बनाना चाहते हैं जो उस परम्परा का पालन नहीं करती है। और उसमें वे अज्ञेय, जैनेन्द्र और कुछ नए लेखकों के साथ स्वयं को भी मानते हैं। बात अगर यहीं तक रह जाती तब भी शायद उतनी बड़ी आपत्ति नहीं होती। क्योंकि इस बात से किसी को बहुत आपत्ति नहीं हो सकती है कि अज्ञेय, जैनेन्द्र और खुद निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा से अलग हटकर अपनी पहचान बनाई थी। हां यहां यह फिर से दुहराया जा रहा है कि प्रेमचंद की परम्परा से हट कर अपनी पहचान बनाने के बावजूद इनमें से कोई भी लेखक शायद यह कहना नहीं चाहेगा किवे ‘बिना प्रेमचंद के भी अपनी लीक बना सकते।’
जैनेन्द्र कुमार का प्रेमचंद से कैसा संबंध था इसे हम सभी जानते हैं। जैनेन्द्र प्रेमचंद का बहुत सम्मान करते थे। और प्रेमचंद ने जैनेन्द्र कुमार को गोर्की की संज्ञा दी थी। इसे इतिहास में पढ़ा और समझा जा सकता है। अज्ञेय पर बोलते हुए जैनेन्द्र कुमार ने इसे साझा भी किया कि प्रेमचन्द की निगाह में जैनेन्द्र क्या थे। जैनेन्द्र इस प्रसंग का जिक्र करते हैं जब वे और अज्ञेय साथ-साथ शांतिनिकेतन जाते हुए काशी रुके थे। वे कहते हैं ‘हम लोग प्रेमचंद के यहां ठहरे थे। वे उन दिनों बीमार थे। वात्स्यायन जी ने तब उनके फोटो भी लिये थे। प्रेमचन्द ने कहीं लिखा था कि जैनेन्द्र में तो गोर्की जैसी प्रतिभा है, लेकिन अज्ञेय भी आगे जाएंगे।’
अज्ञेय, जैनेन्द्र और खुद निर्मल वर्मा को यदि हम देखें तो यह साफ होता है कि वे प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा में ठीक उस तरह से नहीं हैं। यहां सामाजिकता से अधिक व्यक्तिवाद था। यह अलग बात है कि जैनेन्द्र ने हमेशा प्रेमचंद का बहुत सम्मान किया है। भीष्म साहनी ने यूं तो जैनेन्द्र के व्यक्तिवाद को प्रेेमचन्द के यथार्थ से अलग करके देखा है परन्तु उन्होने यह अवश्य लिखा कि जैनेन्द्र के यहां प्रेमचन्द का कितना सम्मान था। जैनेन्द्र कुमार के लिए भीष्म साहनी ने जो लिखा है, उसे इस परम्परा के लेखकों की सोच का आधार माना जा सकता है। भीष्म साहनी सारिका के जैनेन्द्र कुमार विशेषांक में लिखते हैं-‘प्रेमचंद के प्रति उनके (जैनेन्द्र के) दिल में बहुत आदर भाव था। प्रेमचंद के वे बहुत करीब रह चुके थे, प्रेमचंद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था। लेकिन जहां प्रेमचंद सामाजिक-आर्थिक परिवेश को प्राथमिकता देते थे, वहां जैनेन्द्र अपने को उनसे अलग मानते थे।’ आगे वे लिखते हैं ‘गत तीस चालीस वर्षों के हिन्दी साहित्य में दो प्रमुख प्रवृतियां रहीं हैं। एक समाजोन्मुखी, दूसरी व्यक्तिनिष्ठ तथा आत्मकेंद्रित। जैनेन्द्र जी आत्मकेंद्रित प्रवृति के प्रमुख लेखकों में रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि वे सामाजिक जीवन के प्रति उदासीन रहे हैं। उनकी अनेक रचनाओं में सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध, विसंगतियां परिवेश का अंग बनकर आयी हैं। परन्तु सामाजिक प्रश्नों का निदान वे मूलतः व्यक्ति में ही खोजते हैं।’
जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचन्द का संबंध कितना गहरा था इसे जैनेन्द्र के कई लेखों-संस्मरणों से समझा जा सकता है। प्रेमचंद के कई अंतरंग पत्र जैनेन्द्र के नाम हैं जिन्हें पढ़कर उनके बीच के संबंध को समझा जा सकता है। परन्तु फिर भी प्रेमचन्द के लिए दिल में बहुत आदर भाव रखने के बावजूद यह नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए कि कोई लेखक किसी लेखक की नकल हो। जैनेन्द्र कुमार ने एक जगह लिखा है कि प्रेमचन्द खुद नहीं चाहते थे कि जैनेन्द्र उनके जैसा लिखें। चर्चित लेखक गोविंद मिश्र ने इस संदर्भ का उल्लेख अपने आलेख में किया है। वे लिखते हैं- ’बड़े ताज्जुब की बात यह है कि प्रेमचंद जैनेन्द्र की कहानियों के प्रशंसक थे और बकौल जैनेन्द्र उन्होंने जैनेन्द्र को प्रेमचंद जैसा ही लिखने को मना किया था। जैनेन्द्र को अपनी ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया था।’ लेकिन इससे यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि जैनेन्द्र प्रेमचन्द के बिना लीक बना सकते थे या बनाना चाहते थे। साहित्य की एक परम्परा होती है जिसमें कोई महत्वपूर्ण लेखक दूसरे महत्वूपर्ण लेखक की नकल नहीं होता है परन्तु इस परम्परा से बाद की पीढ़ी को बहुत कुछ मिलता है।
प्रेमचंद की सामाजिकता और अज्ञेय का व्यक्तिवाद
अज्ञेय ने अपने यहां समाज की जगह पर व्यक्तिवाद को बहुत महत्व दिया है, और इसे उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं है। अपनी पूरी चिंतन पद्धति में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति से समाज बनता है इसलिए व्यक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे उनके अनेक लेखों के अतिरिक्त उनकी कविता ‘नदी के द्वीप’ और ‘यह दीप अकेला’ से भी समझा जा सकता है। कविता ‘यह दीप अकेला’ की पंक्ति है- ‘यह दीप, अकेेला, स्नेह भरा/है गर्व भरा मदमाता, पर/ इस को भी पंक्ति को दे दो।’
निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद की परम्परा के समानान्तर एक और पंक्ति बनाने का प्रयास किया और उस पंक्ति में जैनेन्द्र और अज्ञेय को उसमें शामिल करने का निर्णय उनका है। ना जैनेन्द्र कुमार ने और ना ही अज्ञेय ने कभी ऐसा कुछ लिखा है जिससे निर्मल वर्मा की इन बातों की पुष्टि हो सके। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जैनेन्द्र कुमार का लिखने का सलीका प्रेमचंद से भिन्न हो परन्तु ऐसे लेखक की श्रेणी में वे भी शामिल नहीं होना चाहेंगे जो स्पष्ट रूप से प्रेमचंद की परम्परा से अपने को अलग कर लें। अज्ञेय को इस पंक्ति में शामिल करने का जो सबसे बड़ा कारण है वह इन तीन शब्दों में छिपा है – परम्परा, संस्कृति ओर स्मृति। निर्मल वर्मा ने अज्ञेय के निधन पर जो आलेख उनकी श्रद्धांजलि के रूप में लिखा उसमें उन्होंने इन बातों को स्पष्ट किया है। निर्मल और अज्ञेय के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे इसका जिक्र उन्होंने उस आलेख में किया भी है परन्तु वे जिन कारणों से अज्ञेय को अपने करीब मानते हैं उनका भी उल्लेख वहां है। निर्मल के सामने सवाल यह नहीं है कि वे अज्ञेय को कितना पसंद करते हैं बल्कि उनके लिए ज्यादा जरूरी यह है कि वे प्रेमचंद के विरोध में समानान्तर रूप से एक पंक्ति तैयार करें और इसलिए वे व्यक्तिगत रूप में अज्ञेय को बहुत अधिक पसंद नहीं करने के बावजूद अज्ञेय से एक खास तरह ही तारतम्यता स्थापित करते हैं। वे पहले अज्ञेय और प्रेमचंद को आमने-सामने भिड़ाते हैं और जैसा कि मैंने ऊपर ही कहा था कि निर्मल के यहां इसके लिए एक गजब की हिचक देखने को मिलती है। निर्मल ने अज्ञेय के यहां गद्य-लेखन में प्रकृति की तीव्र मांसलता को महसूस किया है। और इसे उभारने के लिए निर्मल को पहले इसे स्वीकार करना पड़ता है ‘मैं जो आज तक प्रेमचंद, सुदर्शन और यशपाल की आहार-सामग्री पर पलता आया था, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक सुन्न दुपहर में बालू की तह पर किसी भागती हुई गूजर लड़की की नंगी टांगें सिर्फ अपनी उत्तप्त उदासी में किशोर मन में पहली बार सेक्स की धुंधली चेतना उघाड़ सकती हैं।’ यहां ‘आहार सामग्री’ शब्द पढ़कर बरबस हमें निर्मल का लिखा वह वाक्य याद आता है जहां वे अपने आप को प्रेमचंद की परम्परा से अलग करते हैं।
यह बहुत ही हास्यास्पद है कि अज्ञेय को महान बतलाने के लिए निर्मल वर्मा को अज्ञेय को प्रेमचंद से टकराने की जरूरत पड़ रही है। निर्मल वर्मा लिखते हैं – ‘प्रेमचंद की कहानियों में हम प्रेमचंद को भूल सकते हैं- अज्ञेय हमें हमेशा अपने अस्तित्व की याद दिलाते रहते हैं। अज्ञेय की अधिकांश रचनाओं को पढ़ते हुए बराबर उनकी अदृश्य ‘उपस्थिति’ का एहसास बना रहता है।’ इस ‘उपस्थिति’ शब्द से हमें एक बार फिर से प्रेमचंद के लिए लिखे गए लेख के शीर्षक की याद आती है-‘प्रेमचंद की उपस्थिति’। परन्तु हमें यह समझना पड़ेगा कि अज्ञेय की रचनाओं में अज्ञेय की उपस्थिति को ढूंढ़ने वाले निर्मल वर्मा यहां वाकई उनकी उपस्थिति ही ढूंढ रहे हैं परन्तु प्रेमचंद के यहां उपस्थिति लिखकर भी उनकी अनुपस्थिति। निर्मल वर्मा अपने और अज्ञेय में जो काॅमन ढूंढते हैं वह है -परम्परा, संस्कृति और स्मृति। निर्मल वर्मा मानते हैं कि भारतीय मनुष्य अतीत और परम्परा से उन्मूलित होकर वर्तमान में जी रहा है। उन्होंने अपने आलेख ‘परम्परा और इतिहास बोध’ में स्पष्ट लिखा कि ‘जिन यूरोपीय इतिहासकारों और पुरातत्व के पण्डितों ने सभ्यता से परिचित कराया, उसी सभ्यता ने उस सामाजिक संरचना के तन्तुजाल को भी नष्ट किया, जिसमें मनुष्य अपनी परम्परा में सांस लेता था, अपने पावन अतीत को अपने वर्तमान में जीता था।’ निर्मल वर्मा ने अज्ञेय के यहां जो सबसे बड़ी विशेषता देखी वह थी अतीत और परम्परा को अपने यहां जिन्दा रखने की उनकी चाहत। निर्मल वर्मा ने लिखा-‘मुझे लगता है अपने अंतिम वर्षों में अज्ञेय का अपनी जातीय परम्परा के प्रति आकर्षण- अन्य कारणों के अलावा-इसमें भी था कि वह उसमें उन सब स्मृतियों, मिथकों, पुराणकथाओं को उत्कीर्णित करना चाहते थे जो सैकड़ों वर्षों से हमारी वाचिक और साहित्यिक परंपरा का जीवन-स्रोत रहे हैं। जो काम उनके पिता ने पुरातत्व-क्षेत्र में किया-जमीन से शिलालेख, मूर्तियों को निकालने का कार्य-वही काम अज्ञेय अंतिम वर्षों में अपनी भारतीय अतीत के विशाल स्मृति-प्रदेश में करना चाहते थे, इतिहास की राख-मिट्टी में दबे उन सब ‘मील के पत्थरों’ को खोदकर बाहर निकालना, जिन पर भारतीय संस्कृति के पड़ाव-चिह्न अंकित थे।’ निर्मल वर्मा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को संदेह के घेरे में रखते हुए कहा कि ‘कभी-कभी मैं सोचता हूं कि क्या एक भारतीय बुद्धिजीवी का परंपरा-विरोध उस मानसिक गुलामी के साथ तो नहीं जुड़ा है, जो अंग्रेजों ने पिछले दो सौ वर्षों के दौरान हम पर आरोपित की है, ताकि हम विस्मृति के अंधेरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता के बोझ से छुटकारा पा सकें।’
एक तरफ निर्मल वर्मा अज्ञेय को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वे अतीत में जाकर वहां से अपनी परम्परा और अपनी संस्कृतियों से मोतियों को चुन चुनकर ला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वे भारतीय बुद्धिजीवियों से इसलिए खफ़ा हैं कि उन्होंने अतीत और परम्परा से अपने आपको उन्मूलित कर लिया है। निर्मल वर्मा अपने दोनों प्रयासों में गलत हैं। ना तो अज्ञेय ने टी.एस.इलियट के सिद्धांतों को मानते हुए भी कहीं परम्परा और संस्कृति को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने की बात की है और ना ही भारतीय बुद्धिजीवियों ने परम्परा से उस तरह अपना नाता तोड़ा है।
निर्मल वर्मा यथार्थवाद और व्यक्तिवाद के मुद्दे पर अज्ञेय को प्रेमचंद से अलग मिजाज के लेखक कह देते तो कोई बात नहीं थी। परन्तु अज्ञेय के संदर्भ में प्रेमचंद के लिए जिस तिरस्कार का भाव दिखलाया गया है वह नागवार है। वास्तव में निर्मल को यहां अज्ञेय के लेखन से सीधा मतलब था भी नहीं। निर्मल ने अज्ञेय को जिस कारण पसंद किया है और जिस कारण उन्होंने अज्ञेय को प्रेमचंद की परम्परा से अलग अपनी एक अलग पंक्ति में रखा है उसका कारण वह अतीत प्रेम है जिसमें निर्मल वर्मा बहुत दूर तक निकल गए थे। अपने दर्शन में निर्मल वर्मा का पाश्चात्य संस्कृति से एक खास तरह की नफ़रत और अतीत से एक खास तरह का प्रेम उन्हें एक खास तरह की चिंतन प्रक्रिया में समाहित करता है। निर्मल अपने इस उद्देश्य के लिए अपने चिंतन तक रहते तो कोई समस्या नहीं थी, समस्या तब हुई जब वे इस बहस में बिना बात के प्रेमचंद को खींच लाए हैं।
प्रेमचंद के यथार्थ से रेणु की मुक्ति? (सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा)
प्रेमचंद के यथार्थवादी लेखन से भिन्न लेखन करने के कारण या फिर लिखने के एक खास शिल्प के कारण जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को प्रेमचंद की परम्परा से थोड़ा भिन्न दिखलाना थोड़ी देर तक उलझन पैदा कर सकता है। परन्तु तब बात बहुत उलझ जाती है जब निर्मल वर्मा रेणु को प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा से भिन्न बतलाकर अपनी नई तरह की पंक्ति में शामिल करना चाहते हैं। प्रेमचंद की परम्परा से भिन्न बनती हुई परम्परा में रेणु को रखना उतना सरल नहीं है। इसे स्वीकार करना कि प्रेमचंद से भिन्न परम्परा में रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और खुद निर्मल वर्मा शामिल हो जाएं इसे स्वीकार करना बहुत अटपटा है। निर्मल अपने उसी लेख ‘प्रेमचंद की उपस्थिति’ में आगे लिखते हैं- ‘प्रेमचंदोत्तर पीढी के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों ने अपने अनुभवों को व्यापक औपन्यासिक स्पेस देने के लिए प्रेमचंद के ‘यथार्थवादी’ फाॅर्म से अपने को मुक्त किया है- रेणु के उपन्यास इसका सजीव उदाहरण हैं। प्रश्न यथार्थ से विदा लेने का नहीं था, स्वयं बदलते हुए यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ‘यथार्थवादी’ ढांचे की सीमाओं से मुक्ति पाना था।’ यथार्थ या गैरयथार्थ के मसले पर रेणु क्या अज्ञेय, जैनेन्द्र और निर्मल के करीब बैठ सकते हैं? ऐसा सोचना थोड़ा अजीब लगता है। प्रेमचंद के यथार्थ से रेणु का यथार्थ अलग हो सकता है, उस यथार्थ को प्रस्तुत करने का ढंग अलग हो सकता है। रेणु का शिल्प प्रेमचंद से उन्हें अलग कर सकता है लेकिन क्या वाकई रेणु प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा में फिट नहीं बैठते हैं, यह शायद स्वीकार्य ना हो।
मुक्तिबोध ने प्रेमचंद पर एक छोटा सा संस्मरणात्मक आलेख लिखा था-‘मेरी मां ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया’। इस आलेख में मुक्तिबोध ने प्रेमचंद के लेखन की आत्मा और अज्ञेय, जैनेन्द्र के लेखन के अंदाज को जुदा बतला कर बहुत साफ कर दिया है कि कैसे आगे चलकर प्रेमचंद और रेणु एक परम्परा में समाते हैं। मुक्तिबोध ने अपनी बात को उस तस्वीर को केन्द्र में रखकर शुरू किया है जिसमें प्रेमचंद और प्रसाद एक साथ खड़े हैं। उन्होंने यह माना कि व्यक्तिवाद की शुरुआत प्रसाद से ही होती है जिसमें आगे चलकर जैनेन्द्र और अज्ञेय जुड़ जाते हैं। परन्तु प्रेमचंद इस व्यक्तिवाद से कोसों दूर हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं-‘यह व्यक्तिवाद एक वेदना के रूप में सामाजिक गर्भितार्थों को लिए हुए भी, प्रत्यक्ष, किसी प्रत्यक्ष सामाजिक लक्ष्य से प्रेरित नहीं था। जैनेन्द्र में तो फिर भी मुक्तिकामी सामाजिक ध्वन्यर्थ थे, किन्तु आगे चलकर अज्ञेय में वे भी लुप्त हो गए।’ मुक्तिबोध यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रेमचंद का लेखन किस तरह सामाजिकता और यथार्थवाद पर आधारित था। ‘कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद उत्थानशील भारतीय सामाजिक क्रान्ति के प्रथम और अन्तिम महान कलाकार थे। प्रेमचंद की भाव-धारा वस्तुतः अग्रसर होती रही, किन्तु उसके शक्तिशाली आविर्भाव के रूप में कोई लेखक सामने नहीं आया।’ प्रेमचंद की यह सामाजिकता ही है जो जैनेन्द्र और अज्ञेय को बहुत हद तक उनकी परम्परा से उन्हें अलग करती भी है परन्तु रेणु इस अलग हुई परम्परा में कैसे समा सकते हैं, यह सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है।
रेणु, जिन्हें निर्मल वर्मा अपने साथ करने के लिए प्रेमचंद की परम्परा से अलग कर रहे हैं, ऐसा देखना पड़ेगा कि ऐसा रेणु ने कब कहा या अपने लेखन से उन्होंने कब ऐसा महसूस कराया। प्रेमचंद के लेखन की जिस यथार्थवादी दृष्टि से निर्मल वर्मा रेणु को अलग कर रहे हैं और जिसके लिए ऊपर ही कहा गया है कि यह उनकी शिल्प की भिन्नता तो हो सकती है किंतु यथार्थवादी दृष्टि दोनों की समान है। रामविलास शर्मा ने अपने लेख ‘प्रेमचंद की परंपरा और आंचलिकता’ में रेणु पर लिखते हुए कई ऐसी बातें की हैं जिनसे हम असहमत हो सकते हैं। और इस लेख को पढते हुए हमें साफ-साफ यह भी महसूस हो जाता है कि रामविलास शर्मा, रेणु को लेकर पक्षपाती थे और वे रेणु को लेकर बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। रामविलास शर्मा ने रेणु के शिल्प को चामत्कारिक कहते हुए अनेक ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। रामविलास शर्मा की इस स्थापना से असहमतियों की तमाम गुंजाइश हैं, परन्तु इस पर अलग से बात करने की जरूरत है। लेकिन यहां यह जानना दिलचस्प है कि रामवलिास शर्मा इसी चामत्कारिक शिल्प के आधार पर रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से अलग करते हैं। वे लिखते हैं ‘कथाशिल्प की इन विशेषताओं में ‘मैला आंचल’ का लेखक प्रेमचंद की परंपरा से दूर जा पड़ा है।’ परन्तु साथ ही यहां यह भी जानना आवश्यक है कि जिस रामविलास शर्मा ने इस लेख को इस कदर पक्षपातपूर्ण होकर लिखा है या कहें रेणु को कमतर आंकने के लिए लिखा है वही रामविलास शर्मा रेणु की लाख कमियों को गिनाने के बावजूद रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से अलग करके देख नहीं पाए। अपने उसी लेख में रामविलास शर्मा लिखते हैं ‘फिर भी ‘मैला आंचल’ का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो उसे प्रेमचंद की परम्परा से जोड़ता है। बहुत कम उपन्यासों में पिछड़े हुए गांवों के वर्ग संघर्ष, वर्ग शोषण और वर्ग-अत्याचारों का ऐसा जीता जागता चित्रण मिलेगा। यह उसका सबल पक्ष है। कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके उसके इस गुण को भुला देना उचित न होगा।’ यानि निर्मल वर्मा जिस रेणु को प्रेमचन्द की परम्परा से काटकर एक अलग परम्परा बनाना चाह रहे हैं यानि प्रेमचन्द की यथार्थवादी परम्परा से काटकर एक अलग परम्परा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राम विलास शर्मा रेणु की तमाम कमियां गिनाने के बावजूद भी उन्हें प्रेमचन्द की उस यथार्थवादी परम्परा से अलग नहीं देख पाए।
निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा के समानान्तर एक अलग परम्परा निर्मित कर पहले उसमें जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को शामिल किया फिर अपने आप को। परन्तु यह परम्परा तब तक शायद विश्वसनीय नहीं बन पाती जब तक कि उसमें रेणु शामिल नहीं होते। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित, 1954 में प्रकाशित ‘मैला आंचल’ पर पहली प्रकाशित समीक्षा जब आलोचना के अप्रैल 1955 के अंक में प्रकाशित हुई तब ही उन्होंने लिखा था कि ‘‘मैला आंचल’ गत वर्ष का ही श्रेष्ठ उपन्यास नहीं है, वह हिन्दी के दस श्रेष्ठ उपन्यासों में सहज ही परिगणनीय है। स्वयं मैंने हिन्दी के दस श्रेष्ठ उपन्यासों की जो तालिका प्रकाशित कराई है, उसमें उसे सम्मिलित करने में मुझे कोई कठिनाई न होगी।’ एक तरफ प्रकाशन के महज एक वर्ष के उपरांत अपने समय के महत्वपूर्ण आलोचक के द्वारा यह प्रशंसा और दूसरी तरफ नामवर सिंह की उपेक्षा और रामविलास शर्मा के खुले विरोध ने मिलकर रेणु के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसका फायदा निर्मल वर्मा ने उठा लेना चाहा। नलिन जी ने मैला आंचल की जिस प्रशंसा की परम्परा को शुरू करना चाहा था हिन्दी साहित्य में वह क्रम में काफी दिनों तक चल नहीं पाया। रेणु और मैला आंचल को हिन्दी साहित्य ने लम्बे समय तक एक जबरदस्त उपेक्षा दी। इसी उपेक्षा को अपने पक्ष में करते हुए निर्मल वर्मा रेणु के साथ एक साहचर्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं ‘अब सोचता हूं तो समझ में आता है, हमारी चीजों को चाहे बहुत लोग पढ़ें, किन्तु हम लिखते बहुत कम लोगों के लिए हैं। मैं जिन लोगों को ध्यान में रखकर लिखता था, उनमें रेणु सबसे प्रमुख थे। मैं हमेशा सोचता था पता नहीं मेरी यह कहानी, यह लेख, यह उपन्यास पढ़कर वह क्या सोचेंगे। यह ख्याल ही मुझे कुछ छद्म और छिछला, कुछ दिखावटी लिखने से बचा लेता था।’ वैसे यह सोचने में थोड़ा अजीब अवश्य लगता है कि निर्मल वर्मा के लिखने का जो शिल्प था या उनके लेखन का जो स्फेयर था वह दूर-दूर तक रेणु से साम्य नहीं रखता था। लेकिन निर्मल वर्मा ने अपने और रेणु के बीच एक साहित्यिक पुल निर्माण करने की हरसंभव कोशिश की है।
रेणु और निर्मल के बीच व्यक्तिगत रूप से कितना और कैसा संबंध था यह बहुत ज्ञात नहीं है। जहां तक मुझे ज्ञात है रेणु ने निर्मल वर्मा पर कभी नहीं लिखा है। भारत यायावर द्वारा सम्पादित ‘रेणु रचनावली’ के खण्ड संख्या 5 को जब हम देखते हैं, जिसमें कि रेणु के द्वारा ‘साहित्यकारों पर लिखे गये स्केच एवं संस्मरण’ हैं, हमें वहां यशपाल, अज्ञेय, उग्र, जैनेन्द्र समेत चैदह साहित्यकारों पर उनके द्वारा लिखे संस्मरण मिलते हैं परन्तु वहां निर्मल वर्मा कहीं नहीं हैं। निर्मल वर्मा का भी रेणु पर लिखा सिर्फ एक लेख ही मिलता है- ‘रेणुः समग्र मानवीय दृष्टि’, जिसे उन्होंने रेणु के निधन पर अप्रैल 1977 में लिखा था। मेरी जानकारी में दोनों के बीच कोई पत्र-व्यवहार भी सामने नहीं आया है। ‘रेणु रचनावली’ के इसी खण्ड में रेणु के द्वारा लिखित पत्रों को भी शामिल किया गया है। इन पत्रों में तमाम साहित्यिक वरिष्ठ लेखकों और युवा लेखकों के बीच के पत्र संवाद प्रकाशित हैं परन्तु वहां भी निर्मल वर्मा नदारद हैं। मतलब कुल मिलाकर रेणु की रचनाओं में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा-पढ़ा नहीं मिल पाता है जहां से यह साबित हो सके कि रेणु और निर्मल वर्मा के बीच एक अनौपचारिक सम्बन्ध था।
निर्मल वर्मा ने जब यह लिखा कि वे जो लिखते थे तो सबसे अधिक रेणु को ध्यान में रखकर ही लिखते थे, इससे स्पष्ट होता है कि उनके बीच बहुत ही अनौपचारिक और पारिवारिक सम्बन्ध रहे हों। जबकि निर्मल खुद रेणु के निधन पर लिखे अपने उस इकलौते निबन्ध में अपने सम्बन्ध का जिक्र करते हैं और इससे ऐसा अहसास नहीं होता है कि दोनों के बीच इतना अनौपचारिक सम्बन्ध रहा होगा। निर्मल एक वाकया का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे वे एक बार दिल्ली में एक जुलूस में चल रहे थे और भटकते हुए किसी बिहार के निवासी से मिल लिए और जब बातचीत हुई तो निर्मल वर्मा के यह पूछने पर कि क्या रेणु जी भी आए हैं, उस व्यक्ति ने नहीं के साथ यह सवाल पूछा कि ‘क्या आप उन्हें जानते हैं?’ निर्मल वर्मा ने इस सवाल का जवाब यूं दिया है- ‘यह प्रश्न बहुत देर तक मेरे भीतर गूंजता रहा। मैं उनसे केवल दो-तीन बार मिला था, पर आज भी मैं आंख मूंद कर उनका चेहरा हूबहू याद कर सकता हूं-उनके लम्बे झूलते बाल, एक संक्षिप्त-सी मुस्कराहट, जो सहज और अभिजात सौजन्य से भीगी रहती थी।’ इस प्रसंग के खत्म होने पर एक बार फिर से निर्मल वर्मा लिखते हैं ‘जिस व्यक्ति को केवल एक-दो बार देखा था उसके न रहने से मुझे अपनी लिखने की दुनिया इतनी सूनी और सुनसान जान पड़ने लगेगी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था।’ यहां तक आते-आते यह लग सकता है कि रेणु निर्मल के इतने करीब नहीं थे कि निर्मल वर्मा अपने हर लेखन की प्रतिक्रिया के लिए उनकी तरफ देखें। तब यहां स्पष्ट है कि निर्मल वर्मा ने रेणु के साथ एक ‘मनसा गुरू’ जैसा सम्बन्ध विकसित कर लिया था। वे आगे लिखते हैं -‘रेणु जी का होना, उनकी उपस्थिति ही एक अंकुश और वरदान थी। जिस तरह कुछ साधु-सन्तों के पास बैठकर ही असीम कृतज्ञता का अहसास होता है, हम अपने भीतर धुल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, रेणु जी की मूक उपस्थिति हिन्दी-साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती थी।’ फिर से एक बार समझ लिया जाना चाहिए कि यहां जो रेणु के लिए ‘उपस्थिति’ शब्द आया है प्रेमचंद की उपस्थिति से भिन्न है। रेणु की मूक उपस्थिति भी उपस्थिति है परन्तु प्रेमचंद की उपस्थिति भी अनुपस्थिति। यह ‘मूक उपस्थिति’ वास्तव में वही ‘मनसा गुरू’ वाले सम्बन्ध को द्योतित कर रहा है।
निर्मल वर्मा को रेणु को लेकर जो हिन्दी समाज से गुस्सा है वह उनकी उपेक्षा के कारण। निर्मल लिखते हैं- ‘कितनी बड़ी विडम्बना थी कि मार्क्सवादी आलोचक, जिन्हें सबसे पहले रेणुजी के महत्व को पहचानना था, अपने थोथे नारों में इतना आत्मलिप्त हो गये कि जनवादिता की दुहाई देते हुए सीधे अपनी नाक के नीचे जीवन्त जनवादी लेखक की अवहेलना करते रहे।’ यहां निर्मल की चिन्ता जायज हो सकती है परन्तु नियत नहीं। यह सिर्फ दुश्मन के दुश्मन को दोस्त मानने वाली बात है। आगे देखा जा सकता है- ‘मैला आंचल और परती परिकथा महज उत्कृष्ट आंचलिक उपन्यास नहीं हैं, वे भारतीय साहित्य में पहले उपन्यास हैं जिन्होंने अपने ढंग से, झिझकते हुए, भारतीय उपन्यास को एक नयी दिशा दिखायी थी, जो यथार्थवादी उपन्यास के ढ़ांचे से बिल्कुल भिन्न थी।’ निर्मल वर्मा जिन माक्र्सवादी आलोचकों को इसलिए कोस रहे थे कि इस जीवन्त जनवादी लेखक की उन्होंने उपेक्षा की उनके बारे में आगे अपनी स्थापना दे रहे हैं कि उनके उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास के ढ़ांचे से बिलकुल भिन्न थे। तो क्या मैला आंचल, परती परिकथा एक यथार्थवादी उपन्यास नहीं हैं? तो क्या बिना यथार्थवाद के जनवादिता आ सकती है? तो क्या माक्र्सवादी आलोचकों ने रेणु की उपेक्षा करके सही किया? निर्मल वर्मा रेणु की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि तारीफ के बहाने रेणु के लेखन की जो आन्तरिक शक्ति है उसे ही उन्मूलित कर दे रहे हैं।
अब प्रेमचंद और रेणु के सम्बन्ध पर आखिरी बात। कि आखिर जिस प्रेमचंद की परम्परा से रेणु को हटाकर निर्मल वर्मा एक अलग पंक्ति का निर्माण कर और अपने आप को वहां स्थापित कर एक तरफ प्रेमचंद की आभा को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा से अलग इस पंक्ति से अपने को जोड़कर अपने लेखन की एक खास तरह स्वीकृति चाहते हैं तो सवाल है कि प्रेमचंद की परम्परा पर रेणु का क्या कहना है? क्या वाकई रेणु प्रेमचंद की परम्परा से अपने आप को अलग मानते थे? कथाकार मधुकर सिंह ने रेणु के संग एक बातचीत की है जो ‘रेणु रचनावली’ खण्ड-4 में संकलित है, इसमें इस सवाल का जवाब रेणु ने दिया है कि ‘पिछली पीढ़ी के किन-किन रचनाकारों का लेखन आपको प्रभावित करता है?’ इस सवाल के जवाब में रेणु ने अपने गुरु स्वर्गीय श्री रामदेनी तिवारी ‘द्विजदेनी’ और पूर्णिया के जिला कलेक्टर डब्लू. जी. आर्चर के बाद कुछ साहित्यकारों का नाम यूं लिया है- ‘इनके अलावे जिनका ज्यादा प्रभाव मुझ पर पड़ा है वे हैं- शोलोकोव, तारा शंकर, सीतानाथ भादुड़ी और प्रेमचंद।’ यहां स्पष्ट देखा जा सकता है कि रेणु ने साहित्यकारों में जिनका नाम लिया है उनमें हिन्दी से सिर्फ एक ही लेखक हैं- प्रेमचंद। यह प्रमाण बस यहां रखा जा रहा है ताकि सनद रहे, वरना रेणु के पूरे लेखन में व्यक्त यथार्थ में प्रेमचंद की परम्परा से उनके अलग होने की गुंजाइश कहीं से बचती नहीं है।
प्रेमचंद, यथार्थवाद और निर्मल वर्मा (मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो अरुझाय रे।)
एक बार फिर से यहां निर्मल वर्मा के आलेख ‘प्रेमचंद की उपस्थिति’ की तरफ लौटते हैं। इस आलेख में जो यथार्थवाद की नयी बहस चलायी गयी है उसे एक बार फिर से केन्द्र में लाकर देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतने लम्बे विवाद से निर्मल वर्मा पाना क्या चाहते हैं? कम-से-कम प्रेमचंद के संदर्भ में निर्मल वर्मा को पढ़ते हुए अनायास हमें कबीर का दोहा याद आ जाता है।
मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो है अरुझाय रे।
मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे।
हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद की लोकप्रियता का सबसे बड़ा यूएसपी ही यह है कि वे सबसे अधिक सुलझे हुए लेखक हैं। उनके यहां यथार्थ के विभिन्न रूप हो सकते हैं परन्तु यथार्थ कहीं उनसे छूटते हुए नहीं दिखता। परन्तु निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद के यथार्थ पर ही सवाल खड़े कर दिया है। अपने इस आलेख ‘प्रेमचंद की उपस्थिति’ में शीर्षक इतना सम्मानजनक रखकर निर्मल वर्मा ने इस पूरे आलेख में प्रेमचंद की अनुपस्थिति ही ढ़ूंढ़ने की कोशिश की है। या कम से कम यह प्रयास अवश्य किया है कि उनकी अनुपस्थिति को साबित कर दिया जाए। निर्मल वर्मा के इस आलेख में शुरुआत और अंत में यह आभास होता है कि यह प्रेमचंद की प्रशंसा में लिखा गया लेख है। यह निर्मल का अपना संकोच, हिचक या अपराधबोध भी हो सकता है। या फिर भ्रम फैलाने की एक अजीब तरह की कोशिश भी। क्योंकि शुरू और अंत को अगर छोड़ दिया जाए तो इस आलेख में निर्मल ने अजीब-अजीब तरह से प्रेमचंद की व्याख्या करके प्रेमचंद के पाठकों को भी अजीब से भ्रम में डाल दिया है। निर्मल वर्मा ने अपने आलेख के अंत में यह कहा है कि अगर प्रेमचंद जिंदा होते तो वे भी हँस कर कहते कि भई आप तो मेरी परम्परा में आते हो लेकिन मैं? उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि प्रेमचंद अगर आज जिंदा होते और निर्मल वर्मा का यह लेख पढ़ते तो सोचते कि अरे मेरे लेखन की ऐसी व्याख्या हो सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था।
निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद के पूरे लेखन को कई तरह से विभाजित किया है। एक विभाजन है यथार्थ के स्तर पर सेवासदन की परम्परा और कफन की परम्परा और दूसरा विभाजन है शुरुआत का लेखन और बाद का लेखन। जबवे प्रेमचंद के शुरुआती लेखन पर आते हैं तो उसकी बुराई अपने तरीके से करते हैं तब लगता है कि चलो शुरू के लेखन को बुरा कहा है तो इसका मतलब ही यह है कि अंत का लेखन पसंद है। परन्तु यह क्या, वे तो बाद के लेखन को और भी बुरा कह देते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद कहते हैं कि लेकिन प्रेमचंद इतने महान थे कि वे किस-किस तरह से लेखकोें के बीच उपस्थित हैं, लेखकों को पता तक भी नहीं है। यही उनकी महानता है।
निर्मल, प्रेमचंद के शुरुआती लेखन को यूं खारिज करते हैं ‘यदि ये आरंभिक उपन्यास कमजोर हैं तो इसलिए नहीं कि उनके आदर्श में कोई खोट है, बल्कि असली कमजोरी इसमें है कि उन लिबरल, सुधारवादी आदर्शों का भारतीय यथार्थ की कटु विभीषिका से कोई लेना-देना नहीं था।’ इसे भारतीय बौद्धिको को समझना है कि प्रेमचंद के साहित्य को यथार्थ की कटु विभीषिका से कोई लेना-देना नहीं था। सवाल यह है कि कौन सी विभीषिका है जो प्रेमचंद से छूट गयी है? उत्तर है (प्रेमचंद द्वारा चित्रित किसान को केंद्रित करते हुए) -‘किंतु वह ‘औपनिवेशिक किसान’ था, उसके नीचे दबे भारतीय किसान का मूल चरित्र संस्कृति, धार्मिक आस्था (जो ‘व्यावहारिक धर्म’ से अलग है), मनुष्य प्रकृति और ईश्वर के बारे में उसके परंपरागत विश्वास-उसके सृजन की रोशनी से ऊपर नहीं आते।’ यानि निर्मल का मानना है कि किसानी जीवन की मूल विभीषिका उनकी गरीबी नहीं थी। मूल समस्या थी धार्मिक आस्था, जो नष्ट हो रही थी। और नष्ट कर कौन रहा था?-अंग्रेजी राज।
निर्मल ने पहले ही कह दिया कि प्रेमचंद भी गांधी की तरह सभी समस्याओं को औपनिवेशिक चश्मे से देखना पसंद करते थे। ‘हमें हैरानी होगी कि प्रेमचंद ही नहीं, भारत के अनेक शहरी बुद्धिजीवी- जिनमें स्वयं गांधीजी शामिल थे- (उनके ‘हिन्द स्वराज’ के बावजूद) एक समय में भारतीय समाज की मुक्ति बाहर के दुश्मनों से छुटकारा पाने में खोजते थे- वह चाहे गांधीजी की आंखों में विदेशी सत्ता हो, या प्रेमचंद की आंखों में समाज की कुरीतियां और अंधविश्वास हों, आशा यह थी कि एक बार इनसे छुटकारा पाने के बाद हम दैन्य और दरिद्रता के आंसू भारतीय चेहरे से पोंछ सकेंगे।’ अब चूंकि प्रेमचंद सभी समस्याओं को औपनिवेशिक चश्मे से ही देखते थे तो गरीबी को भी उसी तरह देखा। इस गरीबी के चक्कर में प्रेमचंद अंग्रेजों के द्वारा नष्ट की गई धार्मिक विरासत को पकड़ना ही भूल गए। निर्मल वर्मा लिखते हैं – ‘प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की ‘ऐतिहासिक विकृति’ को देखा था-किंतु उस चीज का मूल सांस्कृतिक टेक्सचर अपने गैर-ऐतिहासिक रूप में क्या था-जो विकृत हुआ था, उसकी अंतदृष्टि प्रेमचंद में नहीं मिलती।’ आगे ‘प्रेमचंद अक्सर उस पक्ष को अनदेखा कर देते हैं, जिसमें भारतीय किसान की सांस्कृतिक विरासत छिपी थी-यह विरासत उसके व्यावाहारिक सामाजिक ‘धर्म’ से कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण थी-एक शब्द में कहें तो उसकी आध्यात्मिक विरासत।’ निर्मल वर्मा की बातें उलझी हुई लग रही हों तो रुककर थोड़ा पहले इसे सुलझा लिया जाए। सरल रूप में निर्मल वर्मा कहना यह चाहते हैं कि प्रेमचंद ने किसानों की समस्या को तो दिखलाया परन्तु मुल समस्या को नहीं। प्रेमचंद ने गरीबी और मजबूरी को दिखलाया परन्तु यह तो एक प्रकार की औपनिवेशिक अंतर्दृष्टि है। जबकि किसानों की मूल समस्या तो है उनसे उनकी आध्यात्मिक विरासत का छूटना। चूंकि अंग्रेजों ने उन्हें यह दिखलाने को मजबूर किया कि किसान गरीब हैं और उन्हें गरीब-मजबूर यहां के भारतीय साहूकार, जमींदार कर रहे थे तो प्रेमचंद ने ‘औपनिवेशिक चश्मे’ के कारण यही दिखलाया। जबकि उन्होंने इस बडे़ सवाल को अनदेखा कर दिया, जो अंग्रेजों के द्वारा किसानों और आम आदमी के बीच की जो धार्मिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत को खत्म करने से उत्पन्न हुई थी। चूंकि प्रेमचंद भारतीय साहूकार की समस्या दिखला रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को नहीं दिखला रहे थे इसलिए प्रेमचंद दोषी हैं। निर्मल वर्मा के अनुसार भारतीय किसान-आम जन के यथार्थ की कटु विभीषिका उनके हाथ से उनके आध्यात्मिक विरासत का छूटना है ना कि उनकी गरीबी। उन्होंने साफ कहा कि प्रेमचंद के लेखन में जो बदलाव आया है वह आदर्शवाद से यथार्थवाद में आया बदलाव नहीं है बल्कि यथार्थवाद को व्यक्त करने के तरीके में आया बदलाव है। यानि प्रेमचंद ने असली यथार्थ को पकड़ा ही नहीं, जिस यथार्थ का वह चित्रण कर रहे थे वह तो अंग्रेजों के द्वारा दिखलाया गया यथार्थ था जिसे एक गुलाम मानसिकता का लेखक अपना होशो-हवास खो कर बस लिख रहा था। निर्मल इसे यूं स्पष्ट करते हैं-‘यह छलांग आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ नहीं थी, जैसा कि हमारे हिन्दी विभागों के प्रोफेसर और आलोचक मानते हैं- कोई भी सच्चा यथार्थ आदर्श से शून्य नहीं होता जैसे कोई भी आदर्श बिना यथार्थ की ठोस अंतदृष्टि के अर्थहीन और बौना हो जाता है, प्रेमचंद के आदर्श नहीं बदले, सिर्फ यथार्थ से उनका संबंध बदल गया।’
किसानों के जीवन में भूख, गरीबी, मजबूरी से बढ़कर कौन सी धार्मिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत होती है, यह तो निर्मल वर्मा ही बतला पाएंगे। और यह कैसी विरासत है जो किसानों की अलग से एक अस्मिता तय करती है। लेकिन यदि यह मान भी लें कि भारतीय आम आदमी की मूल समस्या गरीबी नहीं आध्यात्मिक विरासत का छूटना है और प्रेमचंद ने भारतीय आम आदमी की गरीबी-मजबूरी का उल्लेख किया है। तब भी आगे पढ़कर समझ आएगा कि निर्मल वर्मा अपनी ही बातों में अजीब तरह से उलझे हुए हैं। वास्तव में निर्मल वर्मा को उत्तर पहले से पता है बस वे उस उत्तर को सही साबित करने के लिए सही प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं।
जब यह तय हो गया कि प्रेमचंद को सिर्फ गरीबी ही दिखती है आध्यात्मिक विरासत का छूटना नहीं। तब फिर निर्मल कहते हैं कि प्रेमचंद को गरीबी का चित्रण करना आता ही नहीं था। निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार के एक संस्मरण का उदाहरण देते हुए इसे साबित करते हैं कि प्रेमचंद को धन से बहुत मोह नहीं था। वे जैनेन्द्र के संस्मरण का हवाला देते हुए लिखते हैं- ‘एक जगह वह अपने और प्रेमचंद के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं- ‘मैं अपने को बुद्धि का दुश्मन मानता हूं, जबकि प्रेमचंद के संबंध में कह सकता हूं कि वे धन के दुश्मन थे।’ और जैनेन्द्र कुमार के इस संस्मरण से निर्मल यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि प्रेमचंद धन को ही संदेह की दृष्टि से देखते थे तो उनके लिए धन का अभाव कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और इसलिए प्रेमचंद अपने उत्तरार्द्ध के लेखन में गरीबी को लेकर काफी तटस्थ और ठंडे रहे हैं। वे लिखते हैं -‘मुझे नहीं लगता प्रेमचंद से पहले या बाद के किसी कहानीकार में गरीबी, खासकर हिन्दुस्तानी गरीबी का इतना ठंडा, तटस्थ और तीखा वर्णन मिलता है।’ और आगे- ‘प्रेमचंद चूंकि स्वयं धन को संदेह की दृष्टि से देखते थे, गरीबी के प्रति उनका रुख दया, नफरत और विरोध जैसी भावुक प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग था।’ यानि प्रेमचंद ने धन के अभाव को वरदान माना है। निर्मल को समस्या इस बात से वास्तव में पहुंचना अपने धर्म वाले मुद्दे पर है। उन्होंने कहा -‘धन का अभाव अपने आप में वरदान हो सकता है, अगर वह ऐसी गरीबी को जन्म न दे जिसमें मनुष्य स्वयं अपने धर्म और दायित्व बोध से वंचित हो जाता है।’ यानि प्रेमचंद के यहां धन के अभाव का जश्न तो है परन्तु यहां उनके पात्र अपने धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। निर्मल मानते हैं कि ‘कफन’ कहानी में प्रेमचंद ने घीसू और माधव की गरीबी पर दया कम प्रकट की है बल्कि उन्होंने उनके द्वारा धर्म को नष्ट ज्यादा करवाया है। निर्मल ने कफन को हिन्दी साहित्य की पहली ‘ब्लासफेमस’ कहानी माना है। ब्लासफेमस का शाब्दिक होता है- ईश्वर की निंदा। यानि ऐसी कहानी जो अपने ही धर्म या धार्मिक अनुष्ठान की निंदा कर रही हो। निर्मल धर्म के अतिशय मोह में घीसू-माधव के अमानवीय हो जाने के पीछे के गरीबी के कारण को नहीं देखते। बस उन्हें लगता है कि कफन के पैसे से उन्हें शराब पीते हुए दिखलाने के द्वारा इस कहानी में हिन्दू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गयी है। और यहां तक आते-आते निर्मल वर्मा प्रेमचंद के शुरुआती लेखन को कमजोर साबित करने के बाद अब उनके उत्तरार्द्ध लेखन को भी कमजोर और एक तरह से इस समाज और संस्कृति के लिए निकृष्ट साबित कर देते हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि जब भी वे प्रेमचंद की बाद की रचनाओं को कमजोर साबित करते हैं उसके तुरंत बाद अपने उसी आलेख में अगली ही पंक्ति में लिखते हुए पाए जाते हैं कि प्रेमचंद की उपस्थिति कहां-कहां है और किस तरह उपस्थित हैं।
अब जब कि निर्मल वर्मा ने अपनी ओर से अपनी सारी ऊर्जा प्रेमचंद को नष्ट करने कोशिश में खर्च कर दी, तब सवाल यह बहुत महत्वपूर्ण उठता है कि इसमें निर्मल वर्मा का लक्ष्य क्या है? बहुत ही स्पष्ट रूप में निर्मल दो बातों को जानते हैं कि जब तक प्रेमचंद का साहित्य अपनी ऊष्मा के साथ हमारे साथ हैं प्रगतिशील सोच को कोई दबा नहीं सकता है। प्रेमचंद से हमारी कई मदों में असहमतियां हो सकती हैं परन्तु प्रेमचंद जातिवाद, साम्प्रदायिकता और किसी खास धर्म के झंडे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक प्रेमचंद हैं और प्रेमचंद का साहित्य हैं तब तक साहित्य की अपनी एक जातिवाद विरोधी, सम्प्रदायवाद विरोधी अस्मिता है। यहां धर्म के नाम पर मोबलाइजेशन संभव नहीं है। प्रेमचंद सामंतवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद के सामने चट्टान बनकर खडे़ हैं। यहां प्रेमचंद के साहित्य से अलग हटकर एक प्रसंग का जिक्र उनके निजी जीवन से किया जा सकता है जिनसे प्रेमचंद की पूरी चिंतन प्रक्रिया का पता चलता है। शिवरानी देवी अपनी पुस्तक ‘प्रेमचंद घर में’ में अपनी निजी बातचीत को उद्धृत करती हैं। एक प्रसंग गाय की कुर्बानी को लेकर है। शिवरानी देवी और प्रेमचंद के बीच का यह संवाद है। शिवरानी देवी के द्वारा यह पूछने पर कि गाय की कुरबानी सही कैसे है तब प्रेमचंद इसका जवाब देते हैं- ‘इसका दोषी एक ही वर्ग नहीं है। अगर मुसलमान कुरबानी करता है, एक बूढ़ी-टेढ़ी गाय को लेकर, जिस पर कि दोनों कौमों में झगड़ा होता है, तो जब अंग्रेजों के यहां सैकड़ों गाएं और बछड़े मारे जाते हैं, तब क्यों नहीं हिन्दुओं के खून में गरमी आती? यह कुरबानी में गाय के लिए झगड़ा नहीं होता है, यह दोनों के अंदर एक तरह की कुरेदन रहती है, उसी में पड़कर झगड़ा होता है। कौन-सा देवी का मंदिर है, जहां बकरों की कुरबानी नहीं होती हो? क्या बकरा जीव नहीं है? फिर क्यों बकरे की कुरबानी की जाती है?’ साम्प्रदायिकता के समक्ष प्रतिरोध के इस अंदाज में जब प्रेमचंद खड़ेे हैं तब यह एक खास विचारधारा के लिए कठिनाई अवश्य पैदा करता है।
परन्तु सारे प्रयासों के बावजूद प्रेमचंद के साहित्य को अप्रासंगिक साबित ना किया जा सके तब उपाय क्या है? निर्मल वर्मा अपने पास एक ‘प्लान बी’ भी तैयार करते हैं। और वह है पहले प्रेमचंद के साहित्य में ही यथार्थ के दो पैमाने साबित करना और दूसरा प्रेमचंद के यथार्थवाद से अलग उनके समानान्तर यथार्थवाद की एक नई पंक्ति का निर्माण करना। अब प्रेमचंद के सामने खड़ा करने के लिए एक बड़ा और कद्दावर साहित्यकार भी तो चाहिए तो वे लाते हैं रेणु को। निर्मल जानते थे कि यह काम जैनेन्द्र नहीं कर सकते, अज्ञेय नहीं कर सकते और यहां तक कि खुद निर्मल भी नहीं कर सकते। हिन्दी समाज के द्वारा रेणु की की गई अतिशय प्रशंसा और रेणु की की गई उपेक्षा, दोनों से निर्मल वाकिफ़ थे इसलिए उन्हें रेणु इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी लगे। निर्मल जानते थे कि रेणु का निधन हो चुका है और रेणु का पक्ष लेने वाला कोई उस तरह का धरा नहीं है। इसलिए बहुत आगे तक जाकर उन्होंने रेणु के यथार्थ को अजीब-अजीब तर्क से प्रेमचंद के यथार्थ से अलग किया और उन्हें अपनी पंक्ति का एक तरह से अगुवा घोषित कर दिया।
प्रेमचंद और रेणु: साहित्य में विरोधी नहीं पूरक के रूप में हैं
निर्मल वर्मा यह कहकर कि प्रेमचंद का यथार्थ यूरोप की उन्नीसवीं सदी में विकसित यथार्थवादी ढांचे का यथार्थ है, रेणु को यथार्थ की परम्परा से अलग करते हैं तो वास्तव में बहुत ही साधारण सी बात को उलझा कर प्रेमचंद के सामने अपना या अन्य लेखकों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं जो प्रेमचंद को चुनौती दे सकें। यथार्थ का नया ढंग तलाशते हुए वैधानिकता की तलाश में वे रेणु तक पहुंचते हैं और यहीं आकर वे गलती कर जाते हैं। रेणु का यथार्थ प्रेमचंद के यथार्थ से अलग नहीं है। बस अलग कुछ है तो वह है रेणु का शिल्प। रेणु का अपने विषय को ट्रीट करने का ढंग एकदम अनूठा है। प्रेमचंद का यथार्थ रेणु से होते हुए हम तक पहुंचता है। जिस रेणु को निर्मल वर्मा प्रेमचंद से अलग हटाना चाहते हैं वास्तव में रेणु उस यथार्थ को और विकसित करके उसमें अपने अनूठे शिल्प से चार चांद लगा देते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज जितने प्रेमचंद हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उतने ही रेणु भी हैं। यथार्थ की यह परम्परा प्रेमचंद से चलकर रेणु से होते हुए हम तक पहुंचती है। रेणु उसमें शिल्प का एक नया अध्याय जोड़ते हैं। इसलिए यह सवाल जितना मौजूं है कि आज हम में प्रेमचंद कितने उपस्थित हैं तब सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए हममें रेणु कितने उपस्थित हैैं। प्रेमचंद के साथ-साथ रेणु की उपस्थिति हमारे साहित्य की समृद्धि की निशानी है। निर्मल वर्मा, प्रेमचंद और रेणु को अपने हित के लिए भिड़ाना चाहते हैं परन्तु हमारी प्रगतिशील सोच ऐसी है कि प्रेमचंद और रेणु भिड़ ही नहीं पाते। साहित्य की परम्परा और विरासत के लिए वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, धुर पूरक साबित होकर सामने आते हैं।
प्रेमचंद की प्रासंगिकता और प्रेमचंद की विरासत
राजेन्द्र यादव की एक पुस्तक का नाम है ‘प्रेमचंद की विरासत’। इस पुस्तक में पहला आलेख इसी शीर्षक से है। यह शीर्षक ही अपने आप में इतना मानीखेज है कि इसके लिए कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस पुस्तक का जो दूसरा ओलख है -‘एक सपने की कथा-यात्रा: प्रेमचंद’, इसे अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। राजेन्द्र जी ने इस आलेख में निर्मल वर्मा का नाम तो कहीं नहीं लिया है परन्तु उन्होंने इस आलेख के माध्यम से निर्मल वर्मा ही नहीं बल्कि उन सभी लेखकों-आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है जो प्रेमचंद की उपस्थिति में उनकी अनुपस्थिति ढूंढ़ने का बीड़ा उठाए घूम रहे थे। एक महान लेखक हमारे यहां किस तरह उपस्थित होता है इसका जवाब ढूंढ़ते हुए राजेन्द्र जी अपने निजी जीवन से एक वाकये का उदाहरण लेते हैं। वे अपने पिता की मृत्यु से अपनी बात शुरू करते हैं कि किस तरह उनकी मृत्यु बहुत पहले हो गयी और अब उनका चेहरा भी याद करना मुश्किल है। परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं है उनकी बहुत सी आदतें, बातें, संस्कार उनके अंदर नहीं गयीं। राजेन्द्र जी ने उन बातों का जिक्र किया जो उनमें पिता से आयी हैं और उन बातों का भी जिक्र जो पिता से उन तक नहीं आयीं। ठीक उसी तरह एक महान लेखक की बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती हैं और बहुत सारी बातों से हम असहमत होते हैं लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वे हममें उपस्थित नहीं होते हैं। राजेन्द्र जी लिखते हैं ‘इस तरह, हर क्षण मैं उन्हें अन्वेषित करता हूं, स्वीकार और अस्वीकार करता हूं और इसी द्वंद्वात्मकता में अनजाने ही शायद मेरा अपना अन्तर्व्यक्तित्व बनता रहता है। हां, मैं अपना ‘बाप’ नहीं बनना चाहता, लेकिन स्वीकार-अस्वीकार और अपने समन्वय की प्रक्रिया में उन्हें मैं उपस्थित नहीं पाता, यह कहना गलत है।’ और अगली पंक्ति में एकदम स्पष्ट लिखते हैं- ‘हर बड़ा लेखक, आने वाले के लिए इसी अर्थ में ‘उपस्थित’ होता है।’ यहां उपस्थित को जिस तरह इन्वर्टेड काॅमा में रखा गया है इसका साफ मतलब पता चलता है। और यह भी कि ऐसा लिखकर राजेन्द्र जी किनको जवाब देना चाहते थे।
ऊपर मैंने प्रेमचंद के विरोध को लेकर निर्मल वर्मा की हिचक का जिक्र किया था। मतलब यूं समझा जाए कि प्रेमचंद के विरोध में निर्मल वर्मा एक कदम आगे जाते हैं तो फिर एक कदम पीछे आते हैं और फिर तुरंत दो कदम आगे। निर्मल वर्मा, प्रेमचंद से सिर्फ अपनी असहमति दर्ज कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता परन्तु यहां असहमति नहीं प्रेमचंद का विरोध है। निर्मल वर्मा यह बात बिल्कुल ठीक कहते हैं- ‘किंतु किसी परंपरा को तोड़ना उसकी अवज्ञा करना नहीं है, रेणु, अज्ञेय या जैनेन्द्र यदि बिल्कुल अलग किस्म के उपन्यास लिख पाए तो इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से ही प्रेमचंद मौजूद थे।’ यहां रेणु, अज्ञेय और जैनेन्द्र को एक साथ रखने को लेकर भले ही आपत्ति हो सकती है परन्तु यह बात परम्परा में प्रेमचंद की महत्ता साबित करती है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि प्रेमचंद की विरासत का मतलब अनुकरण होता है। राजेन्द्र जी इसे अपने यहां स्पष्ट करते हैं-‘अनुकरण नहीं, संस्कार के धरातल पर महत्वपूर्ण लेखक, आने वाले लेखकों और पाठकों के लिए पृष्ठभूमि बनता है।’ और आगे -‘इसलिए मैं कतई अपना ‘बाप’ या प्रेमचंद नहीं बनना चाहता। मेरा अपना क्षेत्र शहरी मध्यवर्ग या निम्न मध्यवर्ग है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां मुझे प्रेमचंद को प्रायः रिजेक्ट करना पड़ता है।’ निर्मल वर्मा लिखते हैं -‘तब हमें अचानक पता चलेगा कि स्वयं प्रेमचंद को प्रेमचंद की परम्परा से मुक्त करना जरूरी है।’ यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्रेमचंद को कुछ मदों में रिजेक्ट करने की बात राजेन्द्र यादव भी कर रहे हैं परन्तु राजेन्द्र यादव के ‘रिजेक्शन’ में और निर्मल वर्मा के प्रेमचंद को प्रेमचंद की परम्परा से मुक्त करने में बहुत फर्क है। राजेन्द्र यादव के यहां अपने से वरिष्ठ लेखक के प्रति असहमति है लेकिन निर्मल वर्मा के यहां यह विरोध में तब्दील हो जाती है। राजेन्द्र यादव यहां प्रेमचंद को एक लेखक के रूप में लेखक के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर रहे हैं परन्तु निर्मल वर्मा का विरोध एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में है। सवाल यह है कि प्रेमचंद को प्रेमचंद की परम्परा से मुक्त करने का मतलब क्या हुआ? प्रेमचंद की परम्परा का मतलब क्या है? प्रेमचंद की परम्परा का मतलब है यथार्थ। प्रेमचंद की परम्परा का मतलब है जातिवाद, सम्प्रदायवाद, सामंतवाद का तीक्ष्ण विरोध। प्रेमचंद की परम्परा का मतलब है साहित्य की वह गरिमा जहां वे उसे राजनीति से आगे चलने वाली मशाल साबित करते हैं। प्रेमचंद की परम्परा साहित्य से वह मांग करती है जो उसे जगाए, सुलाए नहीं, क्योंकि और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है।
राजेन्द्र यादव साफ कहते हैं- ‘किसी भी पूर्ववर्ती लेखक की उपलब्धियां नहीं, सरोकार और ‘कन्सर्न’ ही हम ग्रहण कर सकते हैं। अनुकरण या आत्मसात उपलब्धियों का नहीं, सरोकारों का होता है और वही हमें परंपरा से जोड़ते हैं।’ राजेन्द्र यादव जिस सरोकार और कन्सर्न की बात यहां कर रहे हैं निर्मल वर्मा को बस इसी से दिक्कत है। यह गौरतलब है कि ए.आर. देसाई ने एक लम्बा आलेख प्रेमचंद पर लिखा था और उन्होंने उस आलेख की शुरुआत ही इस दुख से की थी कि कैसे प्रतिबद्ध रचनाकारों का विरोध इस समाज में होता रहा है। उन्होंने लिखा ‘जैसा कि अमृत राय ने अपने लेख ‘प्रेमचंद की प्रासंगिकता’ में ठीक ही लिखा है कि प्रेमचंद के जीवनकाल में ही उन्हें ओछा सिद्ध करने की मुहिम चलाई गयी थी। स्वतंत्रता के पश्चात, पचास और साठ के दशक में प्रेमचंद समेत सामाजिक दृष्टि से प्रतिबद्ध सम्पूर्ण लेखक-समुदाय को ओछा सिद्ध करने के लिए व्यवस्थित मुहिम चलाई गई।’ लेकिन इस बात का समापन इससे अवश्य किया जा सकता है कि हमारा समय और जितना कठिन होगा और हमारी नैतिकता का और जितना पतन होगा, प्रेमचंद का विरोध उसी स्तर पर बढ़ता भी चला जाएगा। लेकिन सच यह भी है कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता और जरूरत भी उसी अनुपात में और बढ़ती चली जाएगी।
प्रेमचंद की उपस्थिति और प्रेमचंद की भक्ति का सवाल
अब जब निर्मल वर्मा ने अपने विचार में प्रेमचंद की उपस्थिति को उनकी अनुपस्थिति में बदलने की तमाम कोशिश की है तब बार-बार हम प्रेमचंद की उपस्थिति की तरफ बढ़ते हैं। इतने वर्षों बाद होना तो यह चाहिए था कि प्रेमचंद की उपस्थिति हमारे जीवन में सिर्फ पुरोधा के रूप में होनी चाहिए थी। इस रूप में होना यह चाहिए था कि उन्होंने हमें लिखना सिखलाया, उन्होंने साहित्य के महत्व को समझाया, साहित्य को जीवन से जोड़ना सिखलाया। इस रूप में नहीं होनी चाहिए थी कि प्रेमचंद ने जितने सवाल अपने जीवन में उठाए वे आज कितने प्रासंगिक हैं या वे आज भी कितने मौजूं हैं। लेकिन विडंबना यह है हमारे समाज की कि आज प्रेमचंद एक पुरोधा के रूप में हमारे पास जितने उपस्थित हैं उससे और अधिक अपने उन सवालों के लिए उपस्थित हैं जो उन्होंने अपने समय में उठाए थे। आज हम प्रेमचंद को थोड़ी देर के लिए ही सही, विस्मृत करना चाहें तो उनके द्वारा उठाए गए सवाल हमें ऐसा करने से रोकते हैं। बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि दिनों दिन कठिन होते समय में प्रेमचंद हमारे लिए औैर अधिक प्रासंगिक बनते चले जा रहे हैं।
भीष्म साहनी ने प्रेमचंद की कहानियों का संकलन करते हुए 1987 में लिखा है- ‘जिन मुद्दों को प्रेमचंद ने उठाया था, जिनको लेकर उन्होंने साहित्य-रचना की थी, वे आज भी संगत हैं, उनकी संतुलित वस्तुनिष्ठ दृष्टि आज भी हमें सोचने पर बाध्य करती है, भले ही वह सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक-पद्धति का, समाज के पिछड़े हुए वर्गों का, जात-पांत अथवा स्त्रियों की समस्या हो, प्रेमचंद की दृष्टि, उनके पीछे उनका प्रखर व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता झलकती रहती है।’ 1987 को गुजरे हुए भी तीस वर्ष से अधिक हो गए। लेकिन क्या आज का कोई लेखक यह कह सकता है कि आज से तीस वर्ष से भी पहले भीष्म साहनी ने प्रेमचंद के लिए जो लिखा था उससे रत्ती भर भी सुधार हुआ है। हां लेखक यह लिख सकते हैं कि इन समस्याओं की हालत और बदतर ही हुई है।
प्रेमचंद के जिस यथार्थ से रेणु को अलग करते हुए निर्मल वर्मा ने हिंदी के बड़े हिस्से को उससे अलग किया था उस हिस्से से अलग होना गंभीर साहित्य के लिए संभव नहीं है। एक लेखक के रूप में सारे लेखक यह ख्वाब देखते जरूर होंगे कि प्रेमचंद का जो दारुण यथार्थ है उससे हमारा पीछा छूट जाए परन्तु यह समाज हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। न ही रेणु इस यथार्थ से अलग हो पाए, न मुक्तिबोध, न रघुवीर सहाय, न धुमिल और न ही साहित्य का कोई भी गंभीर लेखक।
निर्मल वर्मा प्रेमचंद की परम्परा को दो तरह से देखते हैं, एक तो यह कि प्रेमचंद की परम्परा में दो परम्पराएं हैं – एक सेवासदन की परम्परा और दूसरी कफन की परम्परा। वे दूसरी बात यह लिखते हैं कि प्रेमचंद खुद भी परम्परा में बंधना नहीं चाहते होंगे। पहली बात पर आएं तो यह सवाल बनता है कि क्या वाकई सेवासदन और कफन की परम्परा अलग थी? अगर निर्मल वर्मा इन दोनांे उपन्यासों की अलग परम्परा बनाने का आधार यथार्थवाद को मानते हैं तो पहले यह मानना होगा कि सेवासदन एक यथार्थवादी उपन्यास नहीं है। तो क्या सेवासदन यथार्थवादी उपन्यास नहीं हैं?
गोदान या कफन में गरीबी का जिक्र है और सेवासदन में सुमन के बेमेल विवाह, दहेज प्रथा और उसके संघर्ष की कहानी है। तो सवाल यह बनता है कि गरीबी के जिक्र से जो परम्परा बनती है, वह एक स्त्री के संघर्ष से यथार्थवाद के स्तर पर अलग कैसे हो जाती है। गोदान में, कफन में गांव है, गरीबी है, जीवन के ऊबड़-खाबड़ रूप हैं तो उसे यथार्थवाद की संज्ञा दी गयी है परन्तु सेवासदन एक स्त्री के जीवन के संघर्ष की कहानी है तो वह निर्मल वर्मा के हिसाब से कफन से अलग कहानी है। घीसू-माधव या होरी से सुमन का संघर्ष अलग कैसे है? रामविलास शर्मा ने होरी और सुमन के संघर्ष को मिला कर देखने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। रामविलास शर्मा लिखते हैं ‘केवल होरी से सुमन की तुलना की जा सकती है।’ आगे उन्होंने होरी के संघर्ष की तुलना सुमन के संघर्ष से करते हुए लिखा है -‘सुमन के संघर्ष और दुखों की गाथा कम रोमांचकारी नहीं है। वह नारी है, इसलिए उसके कष्ट, उसके संघर्ष होरी से दूसरी तरह के हैं।’ यदि बात यथार्थवाद की करें तो रामविलास जी ने सेवासदन को एक नए तरह का यथार्थवाद रचने के लिए याद किया है। वे लिखते हैं- ‘हिन्दी उपन्यासों में यह एक नया यथार्थवाद था, जिसे प्रेमचंद जन्म दे रहे थे।’
ध्यान रहे कि इस नए तरह के यथार्थवाद का आधार रामविलास जी ने ‘सेवासदन’ को माना है।
यहां यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपने से वरिष्ठ रचनाकार की विरासत को स्वीकार करना न तो अपनी नकल है और न ही उनकी भक्ति। प्रेमचंद की विरासत को स्वीकार करने को भक्ति की दृष्टि से देखना एक खास तरह की संकीर्ण मानसिकता है। हिन्दी साहित्य के विकास में प्रेमचंद की विरासत हमारे लिए एक थाती की तरह हैं परन्तु प्रेमचंद और प्रेमचंद के साहित्य से असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। असहमति का मतलब यह कदापि नहीं है कि ‘प्रेमचंद को प्रेमचंद की परम्परा से मुक्त करने की जरूरत है।’ प्रेमचंद के लेखन में प्रगतिशीलता के तमाम बिंदु ढ़ूंढ़ने के बावजूद अस्मितावादी दृष्टि से आलोचना संभव है। प्रेमचंद के साहित्य का स्त्रीवादी पाठ या दलितवादी पाठ प्रेमचंद को कटघरे में रखता है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रेमचंद की विरासत को या प्रेमचंद की परम्परा को यहां अस्वीकारा जा रहा है। प्रेमचंद के लेखन की यह रचनात्मक शक्ति है कि आज का साहित्य प्रेमचंद के साहित्य को विस्मृत करके नहीं उससे टकराकर, उससे संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है।
जिस ‘सेवासदन’ उपन्यास के लिए निर्मल वर्मा को ‘कफन’ के यथार्थ से अलग एक नई परम्परा ढूंढ़नी पड़ रही है, वहीं रामविलास शर्मा ‘सेवासदन’ को एक नए यथार्थवाद की रचना स्वीकार करते है। यहां सुमन और होरी के संघर्ष में भले ही एक साम्य ढूंढने की कोेशिश की जा रही हो परन्तु स्त्रीवादी पाठ से यह सवाल अवश्य उठ सकता है कि आखिर सुमन जब संघर्ष कर रही होती है तब उसके लिए शुचिता का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। सुमन अपने संघर्ष के रास्ते में वेश्यावृति का पेशा अपनाती है परन्तु उसका विवाहित होना, उसके भीतर के संस्कार उसे देह के स्तर पर शुचिता की जकड़न में बांधे रखते हैं।
स्त्रीवादी पाठ के नजरिये से देखें तो मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास ‘चाक’ में सारंग ठीक ऐसे ही पुरुषवाद से संघर्ष करती है परन्तु उसके सामने जब अपनी देह की बात आती है तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करती है। ‘सारंग चुपचाप सेवा कर रही है, या प्यार उंडेल रही है?- मेरा मन जिद्दी है श्रीधर। कहता है, जिस मर्द के साथ तेरे पिता ने विदा कर दिया, उस मालिक से वापिस मांग ले अपनी देह। जीती-जागती इन्द्रियों के संग तो जानवर बेचे जाते हैं। उन्हीं का रस्सा पकड़ाया जाता है।’ शिवमूर्ति लिखित कहानी ‘कुच्ची का कानून’ में नायिका कुच्ची अपनी देह के खुद मालिक होने की बात कहती है। वह अपनी देह से जुड़े हुए निर्णय खुद लेती है और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कुच्ची अपने निर्णय के पक्ष में अपना तर्क देती है ‘जब मेरे हाथ, पैर, आंख, कान पर मेरा हक है, इन पर मेरी मरजी चलती है तो कोख पर किसका होगा, उस पर किसकी मरजी चलेगी, इसे जानने के लिए कौन-सा कानून पढ़ने की जरूरत है?’
सवाल निस्संदेह बनना चाहिए। सवाल तो प्रेमचंद की अन्य रचनाओं पर भी बन सकते हैं। सवाल तो ‘कफन’ और ‘गोदान’ पर भी उठ सकते हैं। लेकिन इससे यह साबित कदापि नहीं हो जाता है कि सेवासदन और कफन की परम्परा अलग-अलग है।
दलितवादी अस्मिता की दृष्टि से देखने पर प्रेमचंद के दलितवादी साहित्य का एक अंतर्पाठ हो सकता है। अनेक दलित साहित्यकारों, विचारकों ने प्रेमचंद की दलित विषयक रचनाओं का एक नया पाठ प्रस्तुत करने की कोशिश की भी हैं।
प्रमुख दलित चिंतक कंवल भारती ने प्रेमचंद पर अपना वक्तव्य देते हुए ओमप्रकाश बाल्मीकि के प्रेमचंद विरोध का समर्थन किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ओमप्रकाश बाल्मीकि द्वारा नागपुर के हिन्दी दलित लेखक सम्मेलन अक्टूबर 1993 में दिए गए वक्तव्य को उद्धृत किया है। बाल्मीकि ने प्रेमचंद पर अपनी राय यूं व्यक्त की है- ‘प्रेमचंद ने दलित चेतना की कई महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। सदगति, ठाकुर का कुंआ, दूध का दाम आदि। लेकिन अंतिम दौर की कहानी ‘कफन’ तक आते आते वे गांधीवादी आदर्शों, सामन्ती मूल्यों, वर्णव्यवस्थाओं के पक्षधर दिखायी पड़ते हैं। एक अंतद्र्वंद्व है उनकी रचनाओं में। एक ओर दलितों से सहानूभूति, दूसरी ओर वर्णव्यवस्था में विश्वास।’ ओमप्रकाश बाल्मीकि के इस कथन का समर्थन करते हुए कंवल भारती लिखते हैं- ‘यही कारण है कि ‘कफन’ एक घटिया कहानी ही नहीं है, यह दलित विरोधी भी है इसके खिलाफ तमाम तर्क दिये जा सकते हैं और दिये गए भी हैं।’ इसे समझना आवश्यक है कि ओमप्रकाश बाल्मीकि ने प्रेमचंद की ‘कफन’ कहानी का विरोध किया है तो अन्य कहानियों का समर्थन भी किया है। कंवल भारती ने भी ‘कफ़न’ कहानी का विरोध किया है तो आगे अपने इसी वक्तव्य में ‘ठाकुर का कुंआ, ‘मन्दिर’, ‘मुक्ति मार्ग’, ‘सद्गति’ कहानी की तारीफ भी की है। कंवल भारती कहते हैं -‘अब, मैं ‘सदगति’ को लेता हूं जिसकी प्रशंसा ओमप्रकाश बाल्मीकि ने भी की है। यह इस दृष्टि से एक अच्छी कहानी है भी कि प्रेमचंद ने इसमें दलित जीवन के यथार्थ को दिखाने में सफलता हासिल की है।’ इस तरह इसे एक स्वस्थ असहमति कहा जा सकता है। यह प्रेमचंद के लेखन को पूर्वग्रह से ग्रसित होकर देखने की कोशिश नहीं है। जहां असहमति है वहां असहमति होना गलत नहीं है।
गांधी-अम्बेडकर विवाद और गांधी के साथ प्रेमचंद
मैं यहां प्रेमचंद के दलित विषयक साहित्य से अलग हटकर प्रेमचंद की वैचारकिता से एक असहमति दर्ज करना चाहता हूं। हां, लेकिन यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेमचंद की वैचारिकता की इस दृष्टि से पहले भी असहमतियां दर्ज की गयी हैं। ओमप्रकाश बाल्मीकि ने प्रेमचंद की दृष्टि में अम्बेडकर को देखने का प्रयास किया था और उन्हंे गांधीवादी करार देते हुए अम्बेडकर के पक्ष में नहीं पाया था। यहां उसी संदर्भ का विस्तार है और इससे यह साबित भी करने का प्रयास है कि असहमति का अर्थ कदापि विरोध नहीं होता है।
संदर्भ पूना पैक्ट का है। इतिहास में यह दर्ज है कि अंग्रेजों के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का दिया गया प्रस्ताव यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी को अस्वीकार था। गांधी के द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्रों के बावजूद जब उपवास का निर्णय लिया गया तब यह देश स्तब्ध रह गया था। 16 सितम्बर 1932 को समाचार पत्र को दिए गए अपने वक्तव्य में लिखा कि ‘चूंकि मेरे उपवास के उद्देश्य के संबंध में कुछ भ्रम फैला जान पड़ता है इसलिए मैं यह बात एक बार फिर कह रहा हूं कि मेरा उपवास ‘दलित’ वर्गों के लिए किसी भी प्रकार के संवैधानिक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के खिलाफ है। ज्यों ही वह खतरा सदा के लिए मिट जाएगा, मैं अपना उपवास तोड़ दूंगा।’ गांधी दलित समाज को हिन्दू समाज का एक अविभाज्य अंग मानते थे इसलिए उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित पृथक निर्वाचन मंडल की योजना उनकी ‘फूट डालो राज करो’ की नीति का एक हिस्सा है। गांधी ने अपने उसी वक्तव्य में स्पष्ट लिखा – ‘किंतु, मेरा तो अस्पृश्यता के हर पहलू से अंतरंग परिचय है और उक्त परिचय मुझे यह मानने को बाध्य करता है कि अस्पृश्यों का जीवन-वह जैसा भी है- उन सवर्ण हिन्दुओं के जीवन से, जिनके बीच और जिनकी सेवा करते हुए वे जीते हैं इस तरह गुंथा हुआ है कि उनको उनसे अलग करना असंभव है। वे एक ही अविभाज्य परिवार के अंग हैं।‘
हम इस बात को जानते हैं कि इस संदर्भ में अम्बेडकर गांधी के सख्त विरोध में खड़े थे। और अनशन के बाद सही मायनों में गांधी का जीवन अम्बेडकर के हाथों में था। अम्बेडकर ने अपने विचारों से समझौता करके गांधी का जीवन बचा तो लिया परन्तु वे ताउम्र इस बात से असहमत रहे कि गांधी ने जो किया और जो उसके लिए तर्क गढ़ा गया वे सही नहीं थे। अम्बेडकर ने इस संदर्भ को स्पष्ट करते हुए लिखा-‘मुझे दो परस्पर विरोधी विकल्पों में से एक को चुनना था। एक आरे मानवता के नाते मेरा कर्तव्य था कि निश्चित मृत्यु से श्री गांधी के प्राणों की रक्षा करूं। दूसरी ओर अस्पृश्यों के लिए उन राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की समस्या थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया था। मैंने मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा की।’ पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध के लिए गांधी के पास अपने तर्क थे और इसके समर्थन के लिए अम्बेडकर के पास। यह तय करना बहुत ही कठिन था कि कौन सही थे।
अम्बेडकर के अनुसार, अस्पृश्यों को ब्रिटिश के द्वारा दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का विरोध हास्यास्पद लगता है। वे लिखते हैं- ‘पृथक निर्वाचक मंडल के विरुद्ध श्री गांधी का तर्क न केवल हास्यास्पद था, बल्कि अनिष्ठापूर्ण भी। श्री गांधी ने पृथक निर्वाचक मंडल पर आपत्ति की क्योंकि इसका अर्थ अस्पृश्यों पर ठप्पा लगाया जाना था। लेकिन संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों में इस ठप्पे से कैसे बचा जा सकता है, यह समझ से परे की बात है। संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र में अस्पृश्यों के लिए सीट के आरक्षण में ऐसा ठप्पा निहित होना ही चाहिए और वह निहित भी है, क्योंकि आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार को नियमानुसार घोषणा करनी ही होगी कि वह अस्पृश्य है।’ पृथक निर्वाचन मंडल जब निरस्त हो गया और संयुक्त निर्वाचन मंडल की स्वीकृति के साथ दलितों के लिए विधान मंडल में आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया तब अम्बेडकर ने इसे दलितों की गुलामी का एक नया अध्याय कहा। डाॅ अम्बेडकर ने संयुक्त निर्वाचन मंडल और पृथक निर्वाचन मंडल की स्थिति की तुलना करते हुए साफ शब्दों में इसपर अफसोस किया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की नीति का पास नहीं होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सीटें आरक्षित तो हुईं लेकिन उन पर अधिकार कांग्रेस का ही रहा तो इसे अम्बेडकर ने कांग्रेस की गुलामी की ही संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा -‘जो अस्पृश्य कांगे्रस में हैं, वे उसकी पूंछ के अंतिम सिरे पर हैं और पूंछ इतनी लम्बी है किवह हिल नहीं सकती।’ वहीं आगे उन्होंने इसका कारण भी स्पष्ट किया -‘वे कांग्रेस में शामिल होने पर विवश क्यों हुए? उत्तर है कि यह सब अनिष्ट संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र प्रणाली के कारण हुआ, जो पूना समझौते की उपज थी।’ अम्बेडकर अपनी जगह कितने सही थे या कितनी दूर दृष्टि थी उनकी, इसे पूना समझौते के पचास वर्ष पूरा होने पर मान्यवर कांशी राम द्वारा लिखित पुस्तक ‘चमचा युग’ (एन एरा ऑफ द स्टूडेज) को पढ़कर समझा जा सकता है। कांशी राम ने इस पुस्तक की रचना का कारण देते हुए अम्बेडकर के इसी तर्क को दोहराया-‘24 सितम्बर 1932 से, जिस तिथि को दलित वर्गों पर संयुक्त निर्वाचन थोप कर और पृथक निर्वाचन छीन कर पूना-समझौता किया गया, चमचा युगा शुरू हो गया। अब जबकि चमचा युग पचास वर्ष की आयु का हो गया है तो पूना-पैक्ट को बड़े पैमाने पर और पूरे भारत में भत्र्सना करने के अलावा इस पुस्तक को लिखने का निर्णय लिया गया।’ आगे ‘इस पुस्तक को जनसाधारण को और विशेषकर कार्यकर्ताओं को सच्चे एवं नकली नेतृत्व के बीच अन्तर को पहचानने की समझ पैदा करने की दृष्टि से भी लिखा गया है।’
डाॅ. अम्बेडकर ने अपने आलेख ‘गांधी और उनका अनशन’ में गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए पत्राचार को शामिल किया है। इस पत्राचार से इस संदर्भ में गांधी के विरोध का कारण भी स्पष्ट हुआ है। गांधी ने पृथक निर्वाचन-मंडल को हानिकर मानते हुए स्पष्ट रूप से लिखा-‘जहां तक हिन्दु धर्म का संबंध है, पृथक निर्वाचक-मंडलों का अर्थ होगा, उसका विखंडन और विनाश।’ गांधी ने आगे अपने पत्रों में इसे और स्पष्ट भी किया और अपने अनशन पर जोर भी दिया- ‘मैं पुनः जोर देकर कहता हूं कि मेरी दृष्टि में यह मामला विशुद्ध धार्मिक मामला है। दलित वर्गों को दो स्थानों पर वोट का अधिकार मिल जाएगा, केवल इस तथ्य से न तो संरक्षण मिल जाएगा और न ही बृहत् हिन्दू समाज टूटने से बच पाएगा। दलित वर्गों के लिए यदि किसी पृथक निर्वाचक-मंडल का गठन किया जाना है तो वह मुझे जहर का ऐसा इंजेक्शन दीख पड़ता है, जो हिन्दू धर्म को तो नष्ट करेगा ही, साथ ही उससे दलित वर्गों का भी रंचमात्र हित नहीं होगा।’
गांधी के विचार को देखें तो यह बहुत ही साफ है कि वे इस पृथक निर्वाचन मंडल की योजना को ब्रिटिश सरकार के एक षड्यंत्र की तरह ले रहे थे। उनका साफ मानना था कि इस तरह हिन्दू धर्म की एकता टूट जाएगी। और इस एकता को तोड़ना ही ब्रिटिश सरकार की मंशा है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं था कि वे दलितों पर हुए और होते आ रहे अत्याचारों का मौन समर्थन कर रहे थे। वे जानते थे कि यह एक जघन्य पाप है परन्तु इसके समाधान के इस रास्ते को वे स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि जब पूना समझौता हुआ तो वे डाॅ. अम्बेडकर के बहुत कृतज्ञ हुए। उन्हें 26 सितम्बर 1932 को समाचार पत्रों को दिए अपने वक्तव्य में विस्तार से इस पर लिखा। ‘यह हृदयों का मिलन है, और मैं एक हिन्दू की हैसियत से एक ओर डाॅ. अम्बेडकर, रावबहादुर श्रीनिवासन और उनके दल तथा दूसरी ओर रावबहादुर एम. सी. राजा का आभारी हूं। वे यदि चाहते, तो तथाकथित सवर्णों को पीढ़ियों के पापों का दण्ड देने के लिए, हठीला और विद्रोही रुख अपना सकते थे। उन्होंने यदि ऐसा किया होता तो कम-से-कम मैं तो उनके रवैये पर रोष प्रकट नहीं कर सकता था और जो अत्याचार हिन्दू समाज के बहिष्कृत लागों पर जाने कितनी पीढ़ियों से होते आ रहे हैं, मेरी मृत्यु उनकी एक बहुत ही तुच्छ कीमत होती।’
अब इस सवाल पर लौटते हैं कि प्रेमचंद से असहमति को ध्यान में रखते हुए पृथक निर्वाचन मंडल पर गांधी और अम्बेडकर के बीच हुए इस विवाद का संदर्भ क्या है। ऊपर के इन लम्बे उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि इस पृथक निर्वाचन मंडल के विषय में गांधी और अम्बेडकर दोनों एक-दूसरे से असहमत थे। दोनों के पास अपने-अपने तर्क थे। दलित समाज के प्रति अगाध श्रद्धा रखने के बावजूद गांधी ने अपने अनशन के द्वारा दलित समाज के प्रतिनिधि डाॅ. अम्बेडकर को झुकने पर मजबूर किया। वहीं अम्बेडकर ने भले ही पूना समझौते पर अपनी सहमति जताते हुए भी हस्ताक्षर कर दिए हों परन्तु वे इस निर्णय से सहमत अंत तक नहीं हुए। अगर इस विवाद पर विचार किया जाए कि दोनों में से सही कौन थे तो यह सवाल पेचीदा हो जाएगा। क्योंकि दोनों के पास अपने-अपने तर्क थे और अपनी-अपनी जगह पर दोनों सही थे। दोनों के विचार में फर्क दलितों के प्रति उनकी निष्ठा के कारण नहीं था बल्कि दोनों की प्राथमिकता के कारण था। गांधी दलितों के साथ सदियों से हो रहे अत्याचार को जानते थे लेकिन वे ब्रिटिशों के षड्यंत्र को भी जानते थे। उनका मानना था कि दलितों के हित के लिए लिए जा रहे इस निर्णय का न तो तरीका सही है और न ही टाइमिंग। वहीं अम्बेडकर मानते थे कि सदियों से संताप झेल रहे दलितों के जीवन में यह उनके महत्व को दिखाने का एक अद्भुत अवसर था।
इतना तय है कि दोनों मनीषियों के पास इस संदर्भ का अपना तर्क है और दोनों से असहमत होना मुश्किल है। प्रेमचंद को एक साहित्यकार-विचारक होने के नाते गांधी और अम्बेडकर के विचारों को बहुत ही तटस्थ होकर विचार करना चाहिए था। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। 1932 के इस वर्ष में गांधी-अम्बेडकर के बीच चला यह विवाद इतना कम चर्चा में नहीं था कि प्रेमचंद को इसके बारे में सम्पूर्ण ज्ञान न हो। प्रेमचंद इतने कम बौद्धिक भी नहीं थे कि उन्हें इन बातों की इतनी समझ नहीं थी। प्रेमचन्द अपने विचारों के प्रति उस समय सक्रिय भी बहुत थे। वे उन दिनों साहित्यिक पत्रिका ‘हंस’ निकाल रहे थे, जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका हो चुकी थी। उस पत्रिका के सम्पादकीय में हर महीने वे समाज के तत्कालीन विषयों पर लिखा करते थे। इसके अतिरिक्त भी वे अन्य पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक तत्कालीन विषयों पर लगातार लिखा करते थे। परन्तु पूना समझौते के आसपास के पूरे लेखन को खंगाल लिया जाए, प्रेमचंद ने कहीं भी अम्बेडकर के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलायी है। उन्होंने जो लिखा है वह गांधी की भक्ति की तरह है। प्रेमचंद के विचार से साफ पता चलता है कि अम्बेडकर की जिद गलत है। और गांधी ने अपने अनशन से इस देश को टूटने से बचा लिया है।
17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पृथक निर्वाचन मंडल का निर्णय लिया गया था और उसके बाद से लगातार गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच इस संदर्भ में पत्राचार होता रहा, जो लगातार प्रचार-प्रसार में रहा। एक महीने की जद्दोजहद के बाद 24 सितम्बर 1932 को पूना समझौता सम्पन्न हुआ। ‘हंस’ का अक्टूबर-नवंबर 1932 के अंक का सम्पादकीय इस विषय पर नहीं है। इस सम्पादकीय का नाम है- ‘नवयुग-2’। 17 अगस्त को आए इस निर्णय के संदर्भ में जो कुछ आलेख प्रेमचंद ने लिखे हैं वे इस प्रकार हैं- 1. साम्प्रदायिक मताधिकार की घोषणा (सम्पादकीय, जागरण, 22 अगस्त 1932), 2. अब हमें क्या करना है (सम्पादकीय, जागरण, 29 अगस्त 1932) 3. महान तप (सम्पादकीय, जागरण, 19 सितम्बर 1932) और हमारा कर्तव्य (सम्पादकीय, जागरण, 26 अक्टूबर 1932)। इन चारों सम्पादकीयों में प्रेमचंद ने सम्मिलित निर्वाचन मंडल के पक्ष में अपने तर्क दिए हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इसे गलत साबित करना भी मुश्किल है, परन्तु चारों सम्पादकीयों में कहीं भी अम्बेडकर का जिक्र तक नहीं आया है और न ही अम्बेडकर के तर्क के साथ कोई सदाशयता ही दिखलाई गई है। तो क्या उस समय डाॅ अम्बेडकर का कद और उनका तर्क इतना छोटा था कि उन्हें ओझल किया भी जा सकता था। क्या अम्बेडकर का तर्क इतना कमजोर था कि वह विचार करने के योग्य भी न हो।
प्रेमचंद राष्ट्रवाद को धार बनाकर अम्बेडकर को ओझल कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा- ‘हमें यह दिखाना है-कि तुम चाहे हमें कितने भी टुकड़ों में बांटों, हम परवाह नहीं करते। हम एक राष्ट्र हैं इस भेद-नीति से हमारी राष्ट्रीयता को कुचलना संभव नहीं है।’ अगले सप्ताह के सम्पादकीय में वे लिखते हैं -‘यदि हमने मताधिकारों के लिए आपस में लड़ाई ठान ली, तो मानों हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार की इस दलील का समर्थन करेंगे, कि भारत में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। जो एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से इतना सशंक हैं, वहां राष्ट्रीयता कहां।’ और जब इस संदर्भ में गांधी ने अपना अनशन शुरू किया तो प्रेमचंद ने इसे ‘महान तप’ की संज्ञा दी और इस अनशन के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले के जागरण का अपना सम्पादकीय इसी शीर्षक से लिखा। प्रेमचंद, गांधी को संत घोषित करते लिखते हैं- ‘धन्य हो महात्मा! राष्ट्र की सेवा में तुम पहले ही अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे। एक प्राण रह गया था। उसे भी राष्ट्र ही की भेंट करने जा रहे हो।’ आगे -‘राष्ट्र पर इस समय जो संकट पड़ा हुआ है, उसका मोचन तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। राष्ट्र की नौका साम्प्रदायिक भंवर में चक्कर खा रही है।’ आगे -‘भारतीय राष्ट का आदर्श मानव शरीर है जिसके मुंह, हाथ, उदर और पांव ये चार अंग हैं। इनमें से किसी अंग के विच्छेद हो जाने से देह अपंग या निर्जीव हो जायगी। हमारे शूद्र भाई इस देह रूपी राष्ट्र के पांव ही कट जायं, तो देह की क्या गति होगी?’ और आगे-‘दलितों के उद्धार का सबसे उत्तम साधन है- सम्मिलित निर्वाचन। यही उनके उत्थान का मूलमंत्र है।’
अपने इस लेख में प्रेमचंद ने दो बार अम्बेडकर को केन्द्र में लिया है, एक बार नाम लेकर और एक बार अप्रत्यक्ष रूप से। नाम इस प्रकार लिया- ‘हम अपने उन अछूत भाइयों को जो हमसे रूठ गये हैं, मनायेंगे, उनके चरणों में गिरकर मनायेंगे। हमें विश्वास है डाॅ. अम्बेडकर और मि. श्रीनिवासन भी राष्ट्र की इस याचना को अस्वीकार न करेंगे।’ और आगे जहां उन्होंने अम्बेडकर के वजूद को मिटाना चाहा-‘हम किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं जानते, जिसने इस एकाग्रता, इस प्रेम और इस उत्साह से दलित-समाज की सेवा की हो। महात्मा उन व्यक्तियों में हैं, जो दलितों के उद्धार में ही हिन्दू जाति के उत्थान और उत्कर्ष का रहस्य छिपा हुआ देखते हैं, जो हिन्दू जाति के मुख से अन्याय के इस कलंक को मिटा देने के लिए अपने प्राणों को भी अर्पण कर देने को तैयार है।’
लेकिन जब गांधी की बारी आयी तो प्रेमचंद के शब्द यूं हैं- ‘हमारी नौका को भंवर से निकालकर पार ले जानेवाला अकेला गांधी है। उसी में वह सामथ्र्य है, वह देवत्व है, वह ऐश्वर्य है। हमें विश्वास है वह ईश्वर के दरबार से हमारे उद्धार का बीड़ा लेकर आया है, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जबवह स्वाधीनता का बीड़ा लाकर जीर्ण और निराश माता को भेंट करेगा।’ इन उद्धरणों को पढ़ने के बाद बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद गांधी और राष्ट्रवाद के पक्ष में थे इसमें कोई बुराई नहीं है परन्तु अम्बेडकर को यूं पूरे विमर्श से ओझल कर देना प्रेमचंद को शक के दायरे में लाता है। हमने यह देखा है कि अम्बेडकर को इस प्रसंग से ओझल करने का काम तो गांधी ने भी कहीं नहीं किया है। गांधी ने हमेशा अम्बेडकर को महत्व देते हुए दलितों के साथ सदियों से हुुए अन्याय को समझते हुए सिर्फ इस तरीके और इस टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक नहीं अनेक जगहों पर यह लिखा है कि अम्बेडकर को उन्हें भला-बुरा कहने का अधिकार है और यदि वे इस पूना समझौता के लिए तैयार नहीं होते तो भी वे उन्हें गलत नहीं कहते। गांधी भी अम्बेडकर के विरोध में खड़े हैं परन्तु उनमें एक गरिमा दिख रही है जो यहां प्रेमचंद में नदारद है। पूना समझौता हो जाने के उपरान्त जो सम्पादकीय प्रेमचंद ने लिखा है उसमें भी सिर्फ गांधी को धन्यवाद दिया गया है अम्बेडकर का कहीं जिक्र तक नहीं है। ‘उस महान आत्मा के अनशन व्रत ने, उसकी तपस्या ने, केवल सात दिनों में यह दिखला दिया कि वास्तव में तपस्या कितनी बलवती होती है। उस महान् आत्मा की तपस्या ने, ब्रिटेन के महान् राजनीतिज्ञों के द्वारा तैयार की हुई उस सुदृढ़ दीवार को, जो हिन्दू अछूतों को अलग करने के लिए बड़े गहन कौटिल्य के सीमेंट में तैयार की गयी थी, विध्वस्त कर दिया।’ यानि निश्चित रूप से हमें अम्बेडकर के इस वाक्य को दुबारा से पढ लिया जाना चाहिए और यह भी समझ लिया जाना चाहिए कि अम्बेडकर को प्रेमचंद ने ओझल करके क्या सही किया है? ‘एक ओर मानवता के नाते मेरा कर्तव्य था कि निश्चित मृत्यु से श्री गांधी के प्राणों की रक्षा करूं। दूसरी ओर अस्पृश्यों के लिए उन राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की समस्या थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया था। मैंने मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा की।’ यहां अम्बेडकर जिसे मानवता कह रहे हैं प्रेमचंद की निगाह में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है।
और अंत में: प्रेमचंद की उपस्थिति है और सदा रहेगी
अब यहां अपने आलेख में अंत में आखिरी बार निर्मल वर्मा के सवाल ‘प्रेमचंद की उपस्थिति’ पर लौटता हूं। प्रेमचंद के तमाम विरोध के बाद अपने आलेख के अंत में निर्मल वर्मा ने जो दिल पर पत्थर रखकर लिखा है, वास्तव में प्रेमचंद वही हैं। निर्मल लिखते हैं-‘किन्तु किसी परम्परा को तोड़ना उसकी अवज्ञा करना नहीं है, रेणु, अज्ञेय या जैनेन्द्र यदि बिल्कुल अलग किस्म के उपन्यास लिख पाए तो इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से ही प्रेमचंद मौजूद थे।’ यह बात बिल्कुल सही है कि प्रेमचंद से असहमत होना उस परम्परा की अवज्ञा नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं या हो सकते हैं जिनको केंद्र में रखकर प्रेमचंद से असहमत हुआ जा सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमचंद से हम कुछ मदों में असहमत होते हैं तो बहुत सारे मदों में स्वतः ही सहमत हो चुके होते हैं। लेकिन यह सहमति निर्मल वर्मा की सहमति की तरह नहीं है- दिल पर पत्थर रखकर। निर्मल जब अगली ही पंक्ति में लिखते हैं-‘यदि हम अपने पुरखों की अपेक्षा कुछ ज्यादा, कुछ अधिक, कुछ महत्वपूर्ण सत्य उपलब्ध करते हैं तो इसका सीधा-सा कारण हैकि हमारी दृष्टि के साथ पुरखों की दृष्टि जुड़ी है- आज जब कुछ समीक्षक और लेखक प्रेमचंद की परंपरा की बात डंके की चोट से दुहराते हैं- उसे कसौटी मानकर आधुनिक-लेखन को प्रगतिशील या प्रतिक्रियावादी घोषित करते हैं, तो मुझे काफी हैरानी होती है। मुझसे ज्यादा हैरानी और क्षोभ शायद प्रेमचंद को होता यदि वह जीवित होते।’ इसलिए मंैने ऊपर दिल पर पत्थर रखने की बात की थी। यह निर्मल वर्मा के अपने मन का फितूर है नहीं तो प्रेमचंद की परम्परा की बात कोई लेखक प्रेमचंद की नकल के संदर्भ में नहीं लेता है। परम्परा या विरासत हमारी धरोहर होती है, हम उससे प्रभावित होते हैं, सहमत-असहमत होते हैं, उनकी नकल हम नहीं करते हैं। यदि कोई लेखक प्रेमचंद के लेखन की नकल करता तो अवश्य प्रेमचंद को दुख होता परन्तु कोई लेखन प्रेमचंद की विरासत को सहमतियों-असहमतियों के साथ, संघर्षोंे के साथ उनके यथार्थ को जिन्दा रखने की कोशिश करता है तो प्रेमचंद को इसपर गर्व होता, क्षोभ नहीं होता। और जहां तक इस बात की बात करें कि प्रेेेमचंद खुद भी परम्परा में बंधना नहीं चाहते होंगे तो यह समझा जाना चाहिए कि परम्परा में जुड़ने का मतलब परम्परा की नकल करना नहीं होता है। इलियट ने अपने पूरे सिद्धांत में परम्परा को साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बतलाया था। लेकिन उनके यहां परम्परा से जुड़ने का मतलब परम्परा का जड़ समर्थन नहीं था। परम्परा का विरोध करना भी परम्परा की बात करना ही होता है। आज जो लेखक स्वयं को प्रेमचंद की परम्परा में पाते हैं तो क्या वे प्रेमचन्द की नकल कर रहे हैं ? नहीं।
यह सच है कि अगर प्रेमचंद को यह अहसास हो जाता कि कोई प्रेमचन्द की परम्परा से जुड़ नहीं रहा है बल्कि प्रेमचन्द का अंधानुकरण कर रहा है तब प्रेेमचंद अवश्य उसका विरोध करते। प्रेमचन्द की परम्परा यथार्थवाद की परम्परा है, जनवाद की परम्परा है, समाज के दुख-दर्द की परम्परा है, समाज के आखिरी व्यक्ति से जुड़ने की परम्परा है। तो कोई भी उत्कृष्ट साहित्य या साहित्यकार इस परम्परा से अलग होकर अपनी पहचान नहीं बना सकता है। लेकिन इस परम्परा से जुड़ने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि प्रेमचन्द ने जो लिख दिया है सिर्फ उन्हीं समस्याओं, घटनाओं पर लगातार लिखा जाए। प्रेमचन्द खुद भी यह नहीं चाहते थे। और इस तरह प्रेमचन्द हमारे बीच उपस्थित हैैं और सदा रहेंगे परन्तु एक नकल की तरह नहीं, हमेशा एक आदर्श की तरह।
सिर्फ निर्मल वर्मा ही नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा लगी हुई है प्रेमचंद के लेखन को कमजोर करने में। परन्तु प्रेमचंद हैं कि हर समय और अधिक और अधिक प्रासंगिक होते ही जाते हैं। निर्मल वर्मा तो एक खास विचारधारा के बहुत ही नर्म नुमांइंदे हैं और यही कारण है कि वहां एक खास तरह की हिचक भी है। नहीं तो आज एक पूरी विचारधारा प्रेमचंद को सनातनी हिन्दू साबित करने पर लगी हुई है। परन्तु यह बहुत ध्यान देने की बात है कि प्रेमचंद के विरोध में एक खास विचार को प्रश्रय देते हुए निर्मल वर्मा जैसे लेखक ही थे जो इतने स्पष्टीकरण की जरूरत भी पड़ी नहीं तो प्रेमचंद का विरोध तो रूढ़िवादियों ने सदा से किया है और आगे भी करते ही रहेंगे और तब किसी को भी न तो स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ी थी और न ही विरोध करने की। यहां निर्मल वर्मा को भी जवाब देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वे अपने विरोध को भीतर छिपाकर मैदान में उतरे थे, जिन्हें उद्घाटित करना आवश्क था। और दूसरी बात यह कि वे एक साथ दो महान लेखकों की आभा को कम करने की कोशिश करते हुए यहां दिखते हैं। सीधे-सीधे प्रेमचंद को और घुमाकर रेणु को। अपने पाले में रेणु को करना रेणु की ऊष्मा को खत्म करने की कोशिश जैसा ही है। प्रेमचंद और रेणु के बीच यथार्थ के धरातल पर फांक पैदा करना रेणु के लेखन के भीतर की आग को मारने जैसा ही है। निर्मल वर्मा लेखक के रूप में चाहे जितने भी महान हों परन्तु चिंतन के स्तर पर वे एक रूढ़िवादी-अतिवादी विचारधारा के बहुत करीब हैं। इसलिए हमें निर्मल के विरोध को समझना चाहिए और निर्मल के बाद इस विचारधारा में आए उबाल को भी समझना चाहिए। परन्तु इतना अवश्य सत्य है कि एक खास रूढ़िवादी विचारधारा के साथ निर्मल वर्मा हों या फिर बाद की पूरी रूढ़िवादी-जातिवादी-सम्प्रदायवादी-फासीवादी परम्परा, जितना ही प्रेमचंद पर आक्रमण करेगी प्रेमचंद की उपस्थिति हमारे बीच और मजबूती के साथ बनी रहेगी। समाज में कट्टरता जितनी बढ़ेगी, प्रेमचंद की उपस्थिति, प्रेमचंद की प्रासंगिकता भी उतनी और बढ़ेगी।
(प्रिय पाठक, पल-पल के न्यूज, संपादकीय, कविता-कहानी पढ़ने के लिए ‘न्यूज बताओ’ से जुड़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

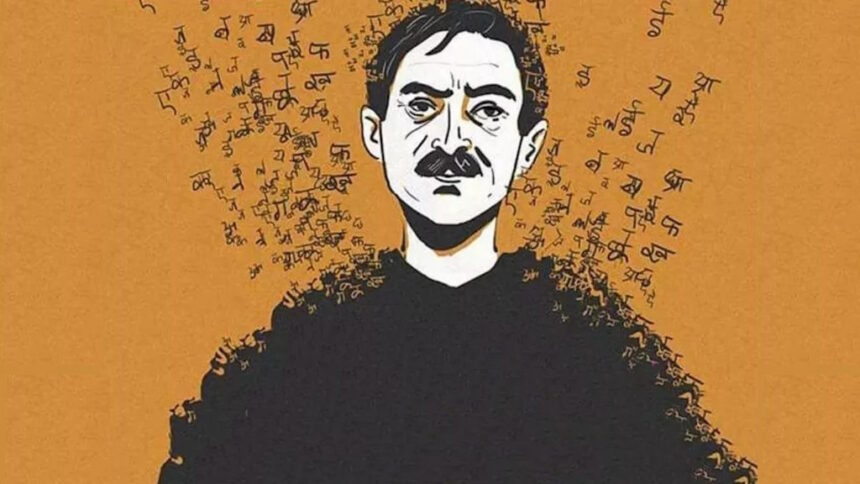
Leave a Reply